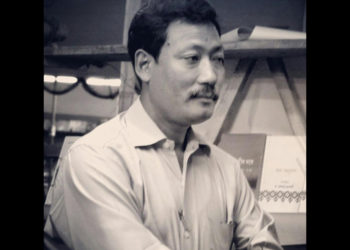एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आज़ादी के 75 वर्ष का ज़श्न मनाने के लिए हमें एक क्षण ठहरना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि क्या हमने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है जिसे हमने 1947 में उस वक़्त निर्धारित किया था जब हमने स्वयं को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र-राष्ट्र में तब्दील किया था। भारत अब रियासतों का समूह नहीं था, जैसा कि वह उपनिवेश होने से पहले था, और भारत के लोग ब्रिटिश राजशाही के अधीन नहीं थे। अब हम एक संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य थे जिसकी आबादी स्वतंत्र और स्वायत्त नागरिकों से युक्त थी, जो किसी के अधीन नहीं थे।
स्वतंत्रता की चाह में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ने भारतीयों को एकजुट किया था, जिससे हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। एक नए समाज के रूप में जो हम राजनीतिक रूप से चाहते थे वह था धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र-राज्य। यह संविधान में अंतर्निहित है, जिस पर सभी की सहमति थी, और जिसकी स्वीकार्यता को हम गणतंत्र दिवस पर याद करते हैं और उसका ज़श्न मनाते हैं। आज प्रश्न यह उठता है कि संविधान ने हमारे जिस राष्ट्र की नींव के रूप में जिसकी संरचना की थी क्या उसे हम व्यवहार में ला सके। हमारी प्रत्येक सरकार जिस संविधान को बनाए रखने की शपथ लेती है; हमें यह पूछना है कि उस संविधान के किस भाग को अक्षुण्ण रखा जा रहा है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान – यदि उसका सम्मान किया जाता है तो – हमें हमारे राज्य और समाज के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के नकारने के प्रयासों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
संविधान हमसे क्या चाहता है और हम किस हद तक संविधान का पालन करते हैं? संविधान की तीन मुख्य आवश्यकताएं हैं : कि, हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य बनें; कि, हम अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को कमजोर किए जाने के सभी प्रयासों के विरुद्ध उसकी सुरक्षा कर सकें; और, कि, हम तीन आधारभूत संस्थाओं – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, को सशक्त बनाए रखें, ये वे एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्र को व्यवहार में लाया जा सकता है, और इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये स्वायत्त बनी रहें।
नेहरू सरकार का सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार एक दूरदर्शितापूर्ण और साहस से भरा हुआ उत्कृष्ट कार्य था। इसी के कारण हम एक लोकतंत्र बने। पारित होने से पहले विधेयक पर दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, में विस्तृत बहस हुई। नागरिकों के विचारों का शासन की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करना हमारे इतिहास के लिए बिल्कुल नया था। जब तक लोग मात्र प्रजा होते हैं, वे सरकारी आदेशों के प्राप्तकर्ता ही बने रहते हैं। लेकिन जब वे एक नागरिक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब क्या आदेश होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसमें उनका दख़ल रहता है।
विगत कुछ वर्षों में, इस पहलू में एक बदलाव आया है। एक व्यक्ति, एक वोट की औपचारिक प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन इसमें उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न प्रकार की अपरादर्शिता की व्यवस्थाएं जुड़ गई हैं, और इसके साथ ही इसमें चुनावों की पूर्व संध्या पर दल बदलुओं का पहलू भी जुड़ गया है। यहां इस बात की जांच भी करनी चाहिए कि प्रत्येक चुनाव के साथ-साथ हर दल के वित्तीय खर्च में एक बेतहाशा बढ़ोतरी क्यों होती है। दोनों ही सदनों में विधेयकों को मात्र औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत करके, और बहुत थोड़ी-सी बहस के साथ पारित कर देना एक रोजमर्रा की बात होती जा रही है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है।
सदियों से, कार्यपालिका – और विशेष रूप से प्रशासनिक सेवाएं और पुलिस – भारत में सभी राज्य व्यवस्थाओं का लौह-द्वार रही हैं। पूर्वकालीन पाठ (टेक्स्ट्स) शासक के सात अंगों को उल्लिखित करते हैं जो इस प्रकार हैं – मंत्री या प्रशासक, संप्रभुता की रक्षा करने वाले बल, खजाने को भरने के लिए करों का संग्रहण, दोस्ताना सहयोगी, किलेबंदी और अधिकार क्षेत्र। मौर्यों से लेकर चोलों और मुगलों तक जिन चीजों पर व्यवहारिक रूप से बल दिया गया था वे थे सशस्त्र बल रखना, पर्याप्त वित्त और एक यथोचित प्रशासन। अशोक मौर्य इसलिए विशिष्ट थे, क्योंकि उन्होंने यह घोषणा की थी कि उनका शासन उनकी प्रजा की बेहतरी के लिए निर्देशित था। अधिकांश सभी शासक जिन्हें हम एक आदर्श के रूप में देखते हैं, जैसे गुप्त, चोल और मुगल, सभी ने इसको लेकर कुछ विशिष्ट निर्देश दिए। शासन नियमित रूप से कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर निर्भर था।
पूर्व आधुनिक समयों में, सम्राट का प्रशासन और पुलिस बल प्रजा के साथ जिस प्रकार व्यवहार करते थे, और कभी-कभी उनके विरुद्ध निर्मम शक्ति का प्रयोग किया जाता था, उसे लेकर बहुत कम शिकायतें होती थीं। राष्ट्र-राज्य के उदय के साथ ही यह सब बदलना ही था। तकनीकी रूप से, अब नागरिक के पास कार्यपालिका की एजेंसियों द्वारा किए गए किसी भी अन्याय या दुर्व्यवहार के विरुद्ध आपत्ति जताने का अधिकार है। यह बात और है कि छोटी जाति की स्थिति और आधी से ज्यादा आबादी की बदहाल गरीबी के चलते कार्यपालिका की संस्थाओं का डर अधिकांश लोगों में बना हुआ है।
पूर्व के समय में, रिसायतों के पास न्यायिक अधिकारी होते थे। उनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता था कि सरकारी आदेशों का पालन हो और आदेशों की अवज्ञा करने वालों को दंडित किया जाए। न्यायिक अधिकारियों को विवादों का निपटारा करना होता था, जिनमें से अधिकांश मामले अपराधों से जुड़े होते थे और बहुत कम मामले नागरिक कानूनों को तोड़ने से जुड़े होते थे, चूंकि नागरिक अधिकार बहुत सीमित थे इसलिए इससे संबंधित कानूनों की संख्या भी बहुत कम होती थी।
प्रजा के स्थान पर स्वतंत्र नागरिक के रूप में और सभी नागरिकों के लिए कानूनी समानता की संस्था के रूप में शासन (अथॉरिटी) से प्रश्न करने या उसका विरोध करने के अधिकार ने इस अतीत से अपने को मुक्त कर दिया, यही सामाजिक न्याय की बुनियाद है। आज नागरिक कानून न्यायिक गतिविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नागरिक और न्यायपालिका, दोनों को ही इस बात को पूरी तरह से अपने संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि शासन के लिए इसका क्या अर्थ है।
औपनिवेशक शासन ने एक न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत औपनिवेशिक शासन को आसान बनाने के लिए की थी। लेकिन अथॉरिटी की आलोचना करने की आजादी-जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में राजद्रोह-जैसे अन्य कानूनों के जरिये अधिकारों में कटौती कर दी गई। औपनिवेशक काल में यह कानून राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और आज भी यह वैसे ही जुड़ा हुआ है। चूंकि यह नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर देता है, अतः इसको समाप्त किए जाने की मांग वैध है।
क्या ये तीन संस्थाएं उनके प्रति जवाबदेह हैं जो शासन (अथॉरिटी) में हैं या फिर उन नागिरकों के प्रति, जिनके अधिकारों की रक्षा के लिए इनकी आवश्यकता है? ये हमारे वक़्त के प्रासंगिक सवाल हैं, तब जब नागरिकों को गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना मुकदमे (ट्रायल) के उन्हें अनिश्चितकाल तक जेलों में डाला जा सकता है। जहां बंदी-प्रत्यक्षीकरण के लिए कोई दर्ख़्वास्त नहीं है, और जहां राज्य का दमन बहुत आम बात हो जाती है। भीमा-कोरेगांव मामले पर विचार करें। नागरिकों को गिरफ्तार किए हुए तीन वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, और अभी भी कोई मुकदमा नहीं चला है। शुरुआत में छह गिरफ्तारियां हुई थीं, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 16 हो गई। कोई भी सोच सकता है कि क्या यह मामला सभी आरोपों और गिरफ्तारियों को सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनाए रखने का है।
इन तीनों संस्थाओं को संविधान के अनुसार समाज की भलाई को सुनिश्चित करना है। जब समाज के सभी स्तरों पर नागरिकों को संविधान के तहत अपने अधिकारों और उनके कार्यान्वयन की साफ समझ होती है, तब इन संस्थाओं की कार्य-पद्धति स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावी हो जाती है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बीते 75 वर्षों के दौरान हमारे समाज के सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए था।
स्वतंत्र नागरिक के क्या अधिकार और दायित्व हैं?
राज्य को अधिकारों की गारंटी देनी होती है। नागरिक राज्य के कानूनों का पालन करने की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि ये कानून उनके अधिकारों के प्रतिकूल न जाएं। इस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि हर नागरिक को भोजन, पेयजल और आश्रय निश्चित रूप से मिले। इसे और अधिक कारगार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिले। अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध करना होगा ताकि इन सब अधिकारों को संभव किया जा सके। इन अधिकारों को मात्र चुनावी नारों के रूप में इस्तेमाल करना या फिर ऐसा दावा करना कि ये सब उपकार के कार्यक्रम हैं, पर्याप्त नहीं होगा। इन सभी अधिकारों का कार्यान्वयन होना आवश्यक है, ताकि शासन स्वीकार्य हो सके। इन अधिकारों और इनके कार्यान्वयन के प्रति जागरुकता विधायिका और कार्यपालिका, दोनों की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए।
सभी नागरिकों की सामाजिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से संबंधित सभी अधिकारों के केंद्र में न्यायपालिका है। यह सब नागरिक और राज्य के बीच अच्छे संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन अधिकारों के ठीक से काम करने के लिए सूचना का अधिकार सबसे मूलभूत आधार है। नागरिकों को यह जरूर पता होना चाहिए कि उनके नाम पर क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं और क्या फैसले लिए जा रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं उनकी बेहतरी को सुनिश्चित करती हैं। सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर व्यापक रूप से बहस होनी चाहिए। इसके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम कुछ भी हो, लेकिन एक स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता है। सरकार की कार्रवाइयों पर आलोचनात्मक मत रखने को स्वतः ही राष्ट्र-विरोधी करार नहीं दिया जा सकता; सरकार राष्ट्र नहीं है। भारतीय परंपरा के पूरे इतिहास में असहमति के विचार और कार्रवाइयां उसके एक अभिन्न अंग बने रहे हैं। जो नया है वह यह है कि अब इन अधिकारों और विशेषरूप से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अधिकार के रूप में सूत्रीकरण किया गया है – यह एक ऐसी विशेषता है जो आधुनिक समाज के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि संविधान स्पष्ट करता है। अगर हम एक लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, तो हर नागरिक के पास न केवल ये अधिकार होने चाहिए बल्कि उसे इनकी समझ भी होनी चाहिए। यह कुछ ऐसा है जो अभी भी हमारे करने के लिए बचता है और शायद हम इसकी शुरुआत हाईस्कूल के छात्रों को हमारे संविधान में दिए गए उनके अधिकारों से अवगत कराने से कर सकते हैं।
मैंने जिन तीन संस्थाओं का उल्लेख किया है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का अस्तित्व मात्र उनके काम-काज तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र सभी नागरिकों की समानता की मांग करता है। किसी भी श्रेणी के नागरिकों को दूसरों के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती – भले ही ऐतिहासिक परिपाटी या सांस्कृतिक विरासत कुछ भी दर्शायी गई हो या फिर उसे बहुसंख्यकों के धर्म के रूप में परिभाषित किया गया हो। इसके अलावा, ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे एक न बदलने वाली पहचान कहा जाए और जो सहस्त्राब्दियों से एक ही समुदाय और वंशजों को संदर्भित करती हो। जब इतिहासकार किसी राष्ट्र के सदियों से मौजूद अतीत और वर्तमान की पहचानों के निर्माण का अध्ययन करते हैं, तो दो प्रत्यक्ष तथ्य उभर कर आते हैं : एक, कि सभी पहचानें बहुत सारी विशेषताओं का एक समागम हैं; और दूसरा, कि ये समय के साथ बदलती रहती हैं।
आज जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रह रहे हैं उन सबके पूर्वज प्राचीन काल से बहुत ही मुख़्तलिफ़ पहचान रखा करते थे। हमें मालूम नहीं है कि हड़प्पावासी स्वयं को क्या कहते थे, क्योंकि उनकी भाषा/लिपि को अभी तक समझा नहीं गया है। अस्थि-पंजरों से लिए गए डीएनए के विश्लेषण से प्राप्त आनुवांशिक साक्ष्य से पता चलता है कि ये सब लोग मिश्रित मूल के थे। इनमें से कुछ पूर्वी ईरानी थे और कुछ स्थानीय उत्तरी भारत के थे।
इसके बाद, जो लोग कुलीन समूह के होते थे उन्हें वैदिक पाठों (टेक्स्ट्स) में आर्य के रूप में संबोधित किया गया है, और जो कई अन्य लोगों से भिन्न होते थे उन्हें दास कहकर संबोधित किया गया है। ये पाठ (टेक्स्ट्स) इन दो तरह के लोगों में भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नता पर जोर देते हैं। डीएनए स्रोतों से मध्य एशिया के आनुवांशिक नस्ल का साक्ष्य मिलता है, जिसका प्रवेश उत्तरी भारत में आज से लगभग चार हजार वर्ष पहले हुआ। यह हाल के समय तक मध्य एशिया से उत्तरी भारत में होने वाले अविलंब पलायनों में से प्रथम होगा।
प्राचीन पाठ (टेक्स्ट्स) शकों/स्किथाइयों, कुषाणों, हुणों/हूनों, और तुरुष्कों/तुर्कों के आगमन का उल्लेख करते हैं। कुछ पशुपालकों के छोटे-छोटे समूहों में आए और कुछ व्यापारियों के रूप में आए। बाद में, ये लोग आक्रांताओं की फ़ौज का एक हिस्सा थे या फिर सूफी मिशनों के साथ आए। ये सब लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बस गए। इसके कारण नए धार्मिक संप्रदायों, भाषाओं और समुदायों का उदय हुआ। इनमें से कुछ अंतर-विवाहों और नई विकसित हुई जातियों में से पनपे, जिनके कारण नई पहचानों का उभार हुआ।
पहली शताब्दी सीई के पूर्वाद्ध में बौध धर्म प्रमुख था। लेकिन उस शताब्दी के अंत तक धीरे-धीरे इसका स्थान पौराणिक हिंदू धर्म (हिंदुइज्म) ने ले लिया। इस्लाम ने पश्चिम से अरबों के साथ, उत्तर से मध्य एशियाई तुर्कों के साथ, और पूर्व से विभिन्न लोगों के समूहों के साथ धीरे-धीरे चरणों में प्रवेश किया। जो इस बड़े मिलाप (इंटर-फेस) से आबादी उभरकर आई, वह आनुवांशिक रूप से बहुत ही मिली-जुली थी, विभिन्न भाषाएं बोलती थीं, और अलग-अलग धर्मों का अनुसरण करती थीं, जिनमें से अधिकांश इस अंतर-मिश्रण से ही विकसित हुई थीं।
अरबों को शुरू में यवन कहा जाता था, भारतीय इस शब्द का इस्तेमाल प्रारंभिक हेलेनिस्टिक लोगों के लिए भी किया करते थे, लेकिन बाद में इस शब्द का इस्तेमाल उन सभी के लिए किया जाता था जो पश्चिम से आए थे। संस्कृत स्रोतों में इन्हें ताजिक भी कहा जाता था। वे अरब सागर के आरपार से व्यापारियों के रूप में आए थे और पश्चिम भारत के तट पर बस गए। इन बसासतों ने विविध प्रकार की इंडो-अरब संस्कृतियों और खोजा, बोहरा, नवायत, मप्पिला तथा इस तरह के विभिन्न धार्मिक संपद्रायों को जन्म दिया। भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ जब हिंद महासागर से अन्य क्षेत्रों के लिए व्यापार खुला, तो स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच और भी मेल-मिलाप बढ़ा। अंततोगत्वा, यूरोपीय लोग व्यापार के लिए और ब्रितानवी भारत को उपनिवेशित करने के लिए आए, लेकिन वे यहां नहीं बसे। वे हमारे विविध वंशक्रम और उसके परिणाम स्वरूप भारत की समृद्ध संस्कृति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने हम पर भ्रामक इतिहास थोपा कि भारतीय समाज दो मोनोलिथिक (एकाश्म) धार्मिक समूहों – हिंदू और मुस्लिम – से बना है और भारतीय इतिहास इन दोनों के बीच के निरंतर शत्रुता से भरा हुआ आख्यान है। वास्तव में, यह इसका उलट था। बहुत सारे समूह थे जो लगातार एक-दूसरे से संपर्क में थे और विकसित हो रहे थे। यही विविधता भारत की समृद्ध संस्कृति का कारण थी।
हिंदू शब्द ईरानी हेन्दू शब्द से आया है जो अरबी भाषा में अल-हिंद बना। भौगोलिक अर्थ में इसकी उत्पत्ति सिंधु (इंडस) नदी से जुड़ी हुई है। केवल पंद्रहवीं शताब्दी सीई में यह शब्द इस्लाम के अलावा भारत में प्रचलित धर्मों के संदर्भ में आया। उस समय के संस्कृत पाठों (टेक्स्ट्स) में हिंदू धर्म का उल्लेख नहीं किया जाता था। उस समय दो ही प्रकार की आस्था व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाता है, जैसा कि बहुत पहले से भी किया जाता था – वे थे, ब्राह्मण और नास्तिक – अर्थात पहले वे जो देव में विश्वास करते थे और दूसरे वे जो नहीं करते थे। बताया जाता है कि यही दो व्यवस्थाएं प्रचलित थीं, जहां नास्तिक वे लोग थे जो पौराणिक हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं रहते थे। यह द्वविविभाजन मौर्य काल तक जाता है, लेकिन नास्तिक श्रेणी के घटक बदल जाते हैं। पहले इसमें देव को नकारने वाले बौद्ध और जैन, दोनों ही शामिल थे। और अब इसमें तुरुष्का भी जुड़ गए। यह उन तुर्कों को संदर्भित करता है जो मुसलमान थे, और जो अल्लाह के रूप में ईश्वर पर तो विश्वास रखते थे, लेकिन पौराणिक देवता पर विश्वास नहीं रखते थे। अतः इन्हें भी गैर-आस्थावानों में शामिल कर लिया गया।
गैर-औपनिवेशक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास के स्रोतों पर पुनः नजर डालें, जैसा पिछले पचास वर्षों से बहुत सारे इतिहासकार कर रहे हैं, तो भारतीय समाज का स्वरूप उपनिवेशीय परिभाषा से बिल्कुल अलग नजर आता है। धर्म तब ऐकिक (यूनिटरी) और एकाश्म (मोनोलिथिक) नहीं थे। वे व्यापक रूप से समुदायों और संप्रदायों की निकटता से बने थे, जैसा कि अन्य समाजों में होता था, वहां भी समय-समय पर सह-अस्तित्व और स्थानीय झगड़े होते थे। वे अपने संबंधों को इसी स्तर पर सुलझा लेते थे। पूर्व–आधुनिक काल में कोई अखिल-भारतीय संगठन नहीं थे। न ही वह एक ऐसा समाज था जो कि हर प्रकार के मतभेदों को अहिंक तरीके से सहन करता रहता था, और न तो वह एक ऐसा समाज था जो लगातार हिंसक टकराव करता रहता था। सभी जटिल पूर्व-आधुनिक समाजों की तरह, इसके भी अपने अंतर्विरोध थे, जिसमें से कुछ असहिष्णुता की ओर जाते थे और कुछ सद्भावपूर्ण तरीके से सुलझा लिए जाते थे। लेकिन ये संबंध विविध क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के बीच में थे।
लोगों, भाषाओं और संस्कृतियों का ऐसा अंतर्मिश्रण दुनिया के अधिकांश हिस्सों का ऐतिहासिक अनुभव रहा है। हम सभी के विविध वंशक्रम हैं और समय-समय पर उनका महत्व बदलता रहता है। वर्तमान समय में हमें इसकी जानकारी है, इसीलिए हमें एक ऐसा तरीका खोज निकालना होगा जो हमें इस बहुलता को स्वीकार करने के साथ-साथ इतना सक्षम बनाए कि हम एक साथ रह सकें। एक लोकतांत्रिक जीवन-शैली को चुनना तार्किक भी है और तर्कसंगत भी, क्योंकि किसी भी प्रकार का बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र का विरोध करता है – जैसा कि वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह भारत की प्रकृति है।
राष्ट्रीय आंदोलन के जरिये जो हमने अपने लिए पहचान गढ़ी थी वह यह थी कि हम सर्वप्रथम और सब चीज से ऊपर सबसे पहले भारतीय हैं। हर नागरिक एक भारतीय था और सबके समान अधिकार थे। यह हमारी समकालीन पहचान है। हिंदुओं ने मलेच्छों को अस्वीकार किया था और मुसलमानों ने काफिरों को। लेकिन भारतीय में सभी नागरिक एक भारतीय के रूप में शामिल हो जाते हैं। हमारे समय में और पूर्व-आधुनिक समय में यही एक सबसे बड़ा अंतर है।
हमें एक भारतीय के रूप में अपनी पहचान का सम्मान भी करना होगा और उसे समझना भी होगा। यह पहचान सहिष्णुता के नैतिक मूल्यों और दूसरे के विरुद्ध हिंसा से दूर रहने के तत्वों से बननी चाहिए। नागरिकता के लिए यह समावेशीकरण बहुत जरूरी है और हमारे संविधान के अनुसार आवश्यक भी है। सभी भारतीयों के एक समान अधिकार हैं। हम भारतीयों के एक समूह को भारतीयों के ही दूसरे समूह की हत्या और सर्वनाश के आह्वान करने की अनुमति नहीं दे सकते, चाहे उनका धर्म, भाषा या जाति कुछ भी हो। हम तभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के आजाद नागरिक बन पाएंगे, जब हम नागरिकता और उसे लागू करने का सही अर्थ समझ पाएंगे।
निबंध को अंग्रेजी में यहां पढ़ें।