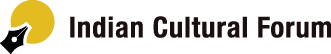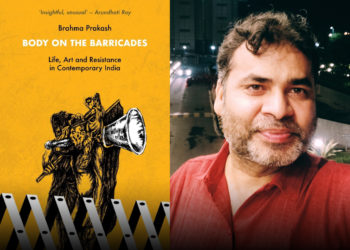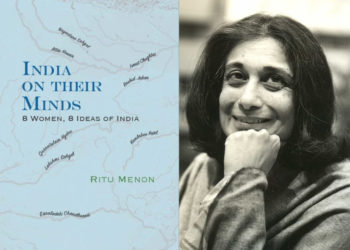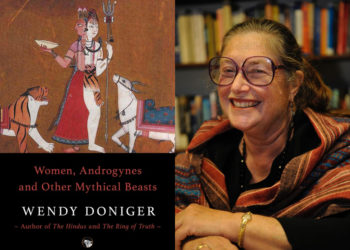गुर्रम जशुवा की लंबी कविता ‘गब्बिलम’ को एक दलित महाकाव्य के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। आधुनिक दक्षिण एशिया पर काम करने वाले इतिहासकार चिन्नैया जंगम ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनके शोध के क्षेत्र में दलित अध्ययन, जाति, और सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास शामिल हैं। वह ‘दलित एंड द मैकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया’ के लेखक हैं।
गुर्रम जशुवा को तेलुगु में दलित साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने ब्राह्मण पंडितों के समतुल्य स्वयं को साबित करने के लिए क्लासिकल तेलुगु में संस्कृत पद का इस्तेमाल किया। ‘गब्बिलम’ में जशुवा अछूतों के अस्तित्व से जुड़ी स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए चमगादड़ के रूपक का इस्तेमाल करते हुए संस्कृत और तेलुगु साहित्य के प्रभावी सिद्धांत को चुनौती देते हैं। चमगादड़ (बैट) या तेलुगु में ‘गब्बिलम’ को एक अपशकुन माना जाता है, चूंकि यह न तो पक्षी है और न ही जानवर। जशुवा क्लासिकल मेघदूत को उलट देते हैं : सवर्णों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संदेशवाहकों हंस, तोता, मोर या बादल के बजाय वह अपशुकनी चमगादड़ का इस्तेमाल करते हैं जो भगवान शिव तक अपनी पीड़ा को पहुंचाने के लिए मंदिर के दुर्गों पर उलटा लटका हुआ है।
भारतीय कविता के क्लासिकल पद-महाकाव्य परंपरा में शायद यह पहली बार है कि गब्बिलम एक दलित व्यक्ति को नायक और मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है; जातिवादी हिंदू समाज में अछूतों के दमन, अलगाव और अमानवीयकरण को दर्शाने वाला यह संभवतः सबसे पहला पाठ है। यह न केवल दलितों की पीड़ा का चित्रण करने में, बल्कि क्लासिकल माध्यम में आम लोगों की भाषा को लाने में तेलुगु साहित्य क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है।
लेखिका गीता हरिहरन के साथ इस वार्तालाप में चिन्नैया जंगम, गब्बिलम एवं दलित महाकाव्य की धारणा और यदि हमें जाति का उन्मूलन करना है तो हमें अभी भी लंबी यात्रा तय की करनी है, उसके बारे में रोशनी डालते हैं।

गीता हरिहरन (जी.एच.) : गब्बिलम, कालिदास के मेघदूत के स्टीरियोटाइप ‘क्लासिकल’ हंस या मोर के बजाय एक चमगादड़ के शीर्षक के जरिये शक्तिशाली रूप से नए सिरे से लिखता है। क्या आप इस पर रोशनी डालेंगे कि यह साहित्यिक युक्ति किस तरह से जाति (और वर्ग) के प्रभाव के प्रत्युत्तर की प्रक्रिया बन जाती है?
चिन्नैया जंगम (सी.जे.) : यह बहुत ही दिलचस्प है कि आपने नए सिरे से लिखने के विचार से शुरुआत की है। गब्बिलम शीर्षक का प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक और सांस्कृतिक सिद्धातों को सिर के बल खड़ा करना है। उनके दोगलेपन को उजागर करके जशुवा यथास्थितिवादी लेखन के प्रत्युत्तर में एक उलट-पलट कर देने वाली युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। प्रभावी रहे ब्राह्मणवादी आख्ययानों के प्रत्युत्तर के रूप में यह शीर्षक उलट-पलट कर देने की इस परियोजना की शुरुआत करता है। यह जाति की वैधता पर सवाल खड़े करता है, और यह अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार और उनके अमानवीयकरण का विरोध करता है।
जी.एच. : मुझे गुर्रम जशुवा की कहानी बहुत ही मार्मिक लगी। गरीबी और जातिवादी भेदभाव में जिंदा रहने के लिए संघर्ष, और साथी कवियों से तिरस्कार एवं उपेक्षा के खिलाफ उनका प्रतिरोध, और सभी प्रकार की रूढ़ियों के खिलाफ प्रतिरोध की कहानी, जो उनके जीवन की कहानी में समाहित है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
सी.जे. : न केवल के एक कवि के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी जशुवा की जिंदगी अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक है। उनके माता-पिता ने अंतर-जातीय विवाह किया था, और उन्होंने जीवनभर गरीबी और भेदभाव का अनुभव किया। एक अछूत होने के नाते जशुवा को संस्कृत, एक शास्त्रीय भाषा जिसे पवित्र और देवों की भाषा माना जाता है, को सीखने से प्रतिबंधित किया गया। जशुवा ने स्वयं ही संस्कृत सीखी, और खुद को ब्राह्मण पंडितों के बराबर साबित करने के लिए उन्होंने संस्कृत के पद के लगभग ही पद रचना की, जिसे उन्होंने क्लासिकल तेलुगु में लिखा। उन्होंने एक थियेटर कंपनी में पटकथा लेखक के रूप में काम किया। लेकिन, क्योंकि उन्होंने संस्कृत का क्लासिकल साहित्य पढ़ा था, तो उन्हें ईसाई मिशनरी स्कूल में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। उन्हें अपने परिवार की मदद के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। उनके पास एक जोड़ी ही कपड़े थे जिसे वह रात में गोदावरी नदी में धोते थे और नदी के किनारे पर सूखाते थे। चूंकि उन्हें रेस्तरां के भीतर जाने की इजाजत नहीं थी, तो उनका एक मित्र रेस्तरां से उनके लिए खाना लाता था। इस तरह के तमाम अपमान झेलने के बावजूद उनके मन में कोई घृणा नहीं थी। उन्होंने कहा कि गरीबी और जातीय भेदभाव ने उन्हें धैर्य सिखाया है, और इसने उन्हें जाति व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोही भी बनाया।
जी.एच. : आपने गब्बिलम को एक दलित महाकाव्य कहा है। गब्बिलम का कैनवास असाधारण रूप से विस्तार लिए हुए है। यह भारत में अलग-अलग वक्तों के इतिहास, उसके विभिन्न धर्मों, सांस्कृतिक व्यवहार और उपलब्धियों, दक्षिण से लेकर उत्तर तक के बदलते भौतिक परिदृश्य, और विविध लोगों, शासकों से लेकर दमित तक, के माध्यम से यात्रा करता है। इसके अलावा भी क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ और विशेषताएं हैं जिनके कारण आप गब्बिलम को एक महाकाव्य के रूप में वर्णित करते हैं? या फिर क्या हम यह देख रहे हैं कि – एक अपशकुनी चमगादड़ के चुनाव के रूप में – साहित्यिक ढांचे को ही तोड़ दिया गया है, चूंकि यह एक दलित महाकाव्य है?
सी.जे. : इस प्रश्न के लिए शुक्रिया। आपने बहुत बेहतर तरीके से इसे सारांशित किया है। निश्चित रूप से यह एक दलित महाकाव्य है, क्योंकि कार्य के कैनवास के हिस्से के रूप में आपने सब कुछ सूचीबद्ध कर दिया है। गब्बिलम पहला दलित पाठ है जो अंतर्मुखी नहीं है, यह दमन के आख्यान के जरिये दलित को स्वयं को परिभाषित करने तक सीमित नहीं है। इसके बजाय, यह भविष्य के अर्थों में और संभावनाओं के अर्थों में दूरंदेशी है। साथ-ही-साथ, यह देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों पर मजबूती के साथ आधारित है। इस विरासत के प्रति इसका दावा इसे एक वास्तविक दलित महाकाव्य के रूप में अनूठा बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह चमगादड़ सहित अधिकतर निंदित/अपशकुनी प्राणियों को दलितों के अस्तित्व संबंधी हालात से जोड़कर समर्थ बनाता है। प्राकृतिक सृजन के सभी पहलुओं का मानवीयकरण करता है और दलित सार्वभौमिकता की शुरुआत करता है। इसलिए मैं इसे एक दलित महाकाव्य कहता हूं।
जी.एच. : भाषा और सत्ता के बारे में गब्बिलम का एक महत्वपूर्ण गूढ़ संदेश है। आपने लिखा है कि जशुवा ने खुद को ब्राह्मणों के बराबर साबित करने के लिए संस्कृत पद का इस्तेमाल सीखा। लेकिन उन्होंने ‘जन भाषा’ (जिसे पढ़ा जा सके और सुना जा सके) के इस्तेमाल के माध्यम से अपने कार्य को सुलभ बनाया। गब्बिलम में जशुवा किसी विदेशी भाषा के बनिस्बत कवियों के लिए बेहतर माध्यम के रूप में मातृ भाषा को एक मुद्दा बनाते हैं। आज हम यह इंगित कर सकते हैं कि हमारी भाषाएं जाति-आधारित हैं। हम स्पष्ट रूप से असंगत विकल्पों के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं?
सी.जे. : बिल्कुल, गब्बिलम के गूढ़ संदेश में या अर्थ में तेलुगु भाषा पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व की जकड़ को चुनौती देना शामिल है। इसीलिए, जशुवा ने ब्राह्मणवादी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्लासिकल परंपरा में लिखने का विकल्प चुना। इसके अलावा, उन्होंने लोगों की आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करके भाषा को ब्राह्मणवादी जकड़बंदी से मुक्त किया, और जो लोग पढ़े-लिखे नहीं थे उनके लिए भी इसे सुलभ बनाया। यह पाठ उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद के संदर्भ में लिखा गया और यह मातृ भाषा एवं राष्ट्र के लिए प्रेम को अभिव्यक्त करता है। उस संदर्भ में, राष्ट्रीय मुक्ति और मातृ भाषा तेलुगु के प्रति लगाव के अभिकथन के संबंध में कोई टकराव नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में सवर्णों के अंग्रेजी भाषा-केंद्रित शिक्षा के प्रति जुनून ने मातृ भाषा में शिक्षा का अवमूल्यन किया। दलित बहुजन इससे बाहर कर दिए गए और उन्होंने खुद को हाशिये पर महसूस किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा जारी रखने का कोई भविष्य नहीं है। यह विडंबना स्थानीय भाषाओं के प्रति सवर्णों के रवैये में निहित है। वर्तमान में भी, अधिकतर क्षेत्रीय भाषाओं में गुंजायमान साहित्य दलित बहुजनों और अल्पसंख्यकों ने ही पैदा किया है; ब्राह्मणवादी अभिजातों ने इस क्षेत्र को बहुत पहले ही छोड़ दिया था।
जी.एच. : हम अक्सर अनुवाद की राजनीति के बारे में बात करते हैं, वह इस अर्थ में कि व्यापक पाठकों/श्रोताओं तक पहुंचने के लिए अनुवाद के लिए क्या चयन किया जाता है। और यह बात यहां भी लागू होती है, क्योंकि जशुवा और योगी वेमना को बहुत-से लोग नहीं जानते हैं, खासकर तेलुगु पाठकों की दुनिया से बाहर। लेकिन आपने अनुवाद की राजनीति के बारे जो लिखा है वह इस बहिष्करण (इक्स्क्लूशन) को एक दूसरे स्तर पर ले जाता है। क्या आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि कैसे गब्बिलम का अनुवाद चाहे वह ‘काव्यात्मक’ था या फिर ‘साहित्यिक’ था, वह इस कविता को उसके राजनीतिक उद्देश्य और अभिव्यक्ति – जातिवाद के खिलाफ उसका क्रोध, प्रतिरोध का जोशीले आख्यान – को चमकाने पर ध्यान केंद्रित कर सका?
सी.जे. : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें औपनिवेशिक इतिहास पर नजर डालनी होगी – जिसमें औपनिवेशिक और ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग ने ब्राह्मणवादी ग्रंथों की प्रशंसा करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया था और सब कुछ ‘हिंदू/भारतीय’ के रूप में परिभाषित किया गया। औपनिवेशिक भारत में अनुवाद का इतिहास ब्राह्मणवादी ग्रंथों को पुनर्जीवित करने के इर्द-गिर्द घूमता रहा। यहां तक कि तेलुगु की तरह की क्षेत्रीय भाषाओं में ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग और औपनिवेशक अभिजात वर्ग ने ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फिर से प्रकाशित किया। मद्रास स्कूल ऑफ ऑरिएंटलिज्म और क्लासिकल तेलुगु की उसकी अनुवाद परियोजनाएं ब्राह्मणवादी ग्रंथों को पुनर्जीवित करने और सांस्कृतिक सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करने पर केंद्रित थी। जशुवा जैसे कवियों को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा – चुनौती के रूप में एक विशिष्ट दलित आवाज प्रस्तुत करने के साथ-साथ क्लासिकल ब्राह्मणवाद के मानकों को पूरा करते हुए कविता लिखना। हाल के वक्त तक शायद ही किसी स्थापित स्कॉलर (विद्वान) द्वारा किसी भी दलित ग्रंथ का अनुवाद किया गया हो। समय आ गया है कि सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से संलग्न सार्थक अनुवाद प्रस्तुत किए जाएं जो कुछ विशेषाधिकार आवाजों के बजाय दमितों की आवाजों पर ध्यान दें।
जी.एच. : जशुवा कविता में कहते हैं, “पुरानी और अज्ञानी परंपराओं की निंदा करो, और शिक्षा को एक दान की तरह फैलाओ।” शिक्षा के अलावा, एक अधिक समतावादी भारत के लिए वह और क्या सुझाते हैं?
सी.जे. : पूरे भारत भर में मुक्ति की दलित परंपरा मुक्ति के एक औजार के रूप में शिक्षा पर विश्वास करती है, और जशुवा इस विश्वास को दमदार तरीके से फिर से दृढ़तापूर्वक कहते हैं। शिक्षा के अलावा, जशुवा राष्ट्र के संसाधानों में बराबर की हिस्सेदारी और शोषण से आजादी एवं गरिमा की मांग करते हैं। वह स्वयं को एक विश्वनारदू, या एक सार्वभौमिक इंसान मानते हैं।
जी.एच. : गब्बिलम ऐतिहासिक और साहित्यिक संकेतों से भरा हुआ है। लेकिन, संभवतः सबसे अहम संकेत जाति-विरोधी परंपराओं के लिए होंगे। क्या आप इन परंपराओं और इतिहासों पर रोशनी डालेंगे जो अक्सर ओझल रहते हैं?
सी.जे. : यदि आप पाठ को ध्यान से पढ़े तो, जशुवा ब्राह्मणवादी ग्रंथों द्वारा जिन जाति-विरोधी परंपराओं को मिटा दिया था, उन्हें सचेत रूप से पुनर्जीवित करते हैं। उदाहरण के लिए, वह पालनती के नायक ब्रह्मा नायडू, जिन्होंने दलितों सहित सभी जातियों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोलने का प्रयास किया था, के बारे में अर्थपूर्ण ढंग से लिखते हैं। जशुवा बौद्ध धर्म के समतावादी नीतिशास्त्र के बारे में बात करते हैं और बुद्ध के बारे में बहुत ही प्रेम से लिखते हैं। तेलुगु ऐतिहासिक संदर्भ में जशुवा जाति-विरोधी कल्पनाओं के बारे में लिखते हैं; पोतुलुरी वीराब्रह्मम और योगी वेमन के बारे में भी लिखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सी.पी.ब्राउन ने वेमन की कवि कर्म को संग्रहित किया और ब्राह्मणों ने इन कविताओं के प्रसार को रोकने का प्रयास किया।
जी.एच. : क्या आप कहेंगे कि जशुवा ने भाषा, लोककथा और विषयों का इस्तेमाल करते हुए गब्बिलम में कवियों के लिए प्रवेशिका जैसा कुछ लिखा है?
सी.जे. : हां, उन्होंने लिखा है। लेकिन उनके रास्ते का अनुसरण करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी कविता क्लासिकल पद में लिखी गई है। कोई और दलित कवि उनकी तरह नहीं लिख सका
जी.एच. : अपनी जाति की वजह से लोगों, जिंदगियों और इतिहासों को खत्म करने के खिलाफ गब्बिलम कविता की एक आवाज को खड़ी करता है। यह कविता 1941 में लिखी गई। वर्तमान में यानी 2022 में हम पाते हैं कि एनसीआरटी की पाठ्य पुस्तकों में जातिगत भेदभाव, जाति-विरोधी शख्सियतों और दलितों की जिंदगियों के विवरणों को काफी कमजोर कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, मैला ढोने वाले, जो निरपवाद रूप से दलित होते हैं, उनके विवरण को हटा दिया गया है और यह भी उस समय किया गया जब मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ ‘स्टॉप किलिंग अस’ अभियान चलाया जा रहा है। समानता की तरफ हमारी यात्रा में इस तरह का यह डिस्कनेकट हमें क्या बताता है?
सी.जे. : सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी के अर्थों में भारत उलटे पांव चल रहा है। हिंदुत्व का आक्रामक हमला बीते 75 वर्षों में जो भी प्रगति की गई है उसे नष्ट कर रहा है। इसके अलावा, भाजपा के मातहत भारतीय राज्य दमन के हर रूप को नकार रहा है। वे महाशक्ति का दर्जा हासिल करने के लिए नींद में चलने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन कुछ दशकों में भारत दलित बहुजनों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण महापरिवर्तन का गवाह बनेगा, क्योंकि उन्हें पीछे छोड़ दिया जा रहा है और ब्राह्मणवाद तथा राज्य एवं वैश्विक पूंजी के अधम गठजोड़ से फल-फूल रहे क्रोनी कैपिटलिज्म, दोनों के ही भार से कुचला जा रहा है।
जी.एच. : उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी कविता के संदर्भ का बहुत ही अहम हिस्सा है (स्वतंत्रता आंदोलन में दलितों की भूमिका पर आपकी पहले वाली किताब से यह बात दिमाग में आती है)। जशुवा ‘स्वतंत्रता के रथ’ के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी पूछते हैं कि ‘क्या स्वतंत्रता के महल में उन्हें जगह मिलेगी।’ वह पूछते हैं, ‘स्वतंत्र भारत में हर समुदाय को क्या हिस्सा हासिल होता है?’ क्या आप वर्तमान भारत में हमारे लिए जशुवा के सवालों की दुखांत अनुगूंज पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
सी.जे. : भारत में दमितों के लिए भविष्य धुंधला दिखता है, चूंकि राज्य अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से पीछे हट गया है और अमीर एवं ताकतवरों के लिए एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। बीते आठ वर्षों में दलित, मुसलमान, आदिवासी और मानवाधिकार के रक्षकों को नफरत और हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। समानता और स्वतंत्रता के लिए अपने अधिकारों का दावा करने वाले लोगों को पहले से कहीं अधिक बहिष्कृत किया जा रहा है और उन्हें अमानवीय दिखाया जा रहा है। इस संदर्भ में गब्बिलम जैसा दलित पाठ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर निर्मित हमारे राष्ट्र की नींव पर खतरे के बारे में हमें चेता रहा है।
कृष्ण सिंह द्वारा हिंदी में अनुवादित। अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ें।