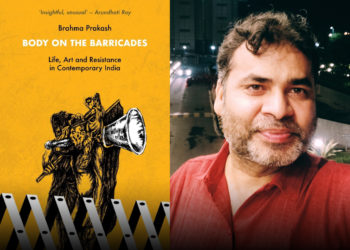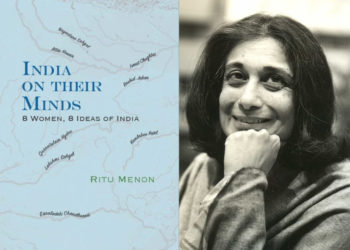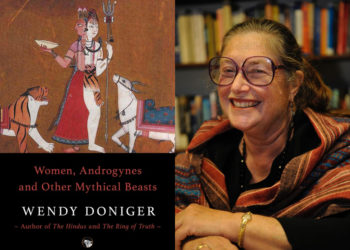रंगमंच निर्देशक और निर्माता सुनील शानबाग का बीते चालीस वर्षों में रंगमंच का कार्य समकालीन भारत की जटिल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने रंममंच के इस कार्य को मंचन के साथ-साथ विभिन्न तरह के वैकल्पिक प्रदर्शनों के माध्यम से अंजाम दिया है। इसमें उन्होंने जिन विषयों को शामिल किया है उनमें वर्ग, जाति, जेंडर और समुदाय द्वारा उत्पन्न असमानताओं की अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं। उनके रंगमंचीय कार्य के संबंध में लेखिका गीता हरिहरन ने उनसे बातचीत की। इस बातचीत का यह पहला भाग है। गीता हरिहरन के साथ इस बातचीत में शानबाग एक ऐसे वक्त में जब कल्पनाशील अभिव्यक्ति के विचारों के लिए एक सुरक्षित रचनात्मक जगह बनाना बहुत मुश्किल से भरा होता जा रहा है, राजनीतिक कर्म के रूप में रंगमंचीय प्रदर्शनों के लिए इस तरह के स्थानों के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही वह यह भी कहते हैं कि मानव सभ्यता के लिए असहमति उसका एक अभिन्न हिस्सा है।

गीता हरिहरन (जी.एच.) : मेरा मानना है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि हमारा कलात्मक व्यवहार राजनीतिक है, लेकिन जो कई तरह के जटिल तरीकों से स्पष्ट नहीं होता है। इस आमफहम सच्चाई का अनुभव हम सबको है, लेकिन हम हर रोज उसे नए सिरे से सीखते हैं, इस पर आपका क्या विचार?
सुनील शानबाग (एस.एस.) : मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वह यह है कि राजनीति ने जो कुछ निर्मित किया है उसकी परिभाषा बीते 15 वर्षों में काफी व्यापक हुई है। कलाओं में पहले की राजनीति की समझ सीमित थी, जो उस समय जाहिर थी, उदाहरण के लिए कहें तो, व्यक्ति और राजनीति के बीच में संबध या फिर राज्य सत्ता के संस्थानों के साथ। मुझे याद आता है कि किसी ने मेरे द्वारा मंचन किए गए एक नाटक के बारे में निराशा का इजहार किया था, अन्य चीजों के अलावा, भारतीय परंपरा में संगीत निर्माण की सांस्कृतिक राजनीति को देखते हुए उनका कहना था कि मेरे पहले के नाटकों की तुलना में इसमें “राजनीति” का अभाव है। या फिर एक और उदाहरण है, जिसमें एक नाटक को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया कि वह पहचान और भाषा को एक राजनीतिक के रूप में देखता है। लोग अभी भी श्रेणियों का निर्माण करते हैं और उसी में अपने का महफूज पाते हैं, और यह निराशाजनक है।
मैं समझता हूं कि इस सबका संबंध देश में बढ़ रहे अ-बौद्धिक माहौल से भी है, जिसका मुख्य धारा की कला पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही है – चाहे वो सिनेमा हो या संगीत हो, या फिर रंगमंच हो। इससे हमें यह समझ आता है कि आज के समय में विचारों और बुद्धिमत्ता के लिए सुरक्षित स्थान बनाना और उसे पोषित करना रेडिकल तौर पर कितना राजनीतिक है! जहां प्रतिबिंबन, विचारशीलता, भिन्न-भिन्न विचारों के लिए सम्मान और विचार-विमर्श तथा बहस चीखने-चिल्लाने या यहां तक कि शारीरिक रूप से हमलों के भय के बिना भी संभव हो सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम समय में पीछे चले गए है। मुझे याद है कि यह बहुत पहले की बात नहीं है जब हमारा उद्देश्य था कि हम रंगमंच की मुख्यधारा में रंगमंच को लेकर अपने विचारों के साथ अपना एक स्थान बनाएं। मौजूदा हालातों में यह असंभव लगता है – यहां तक कि मूर्खतापूर्ण भी लगता है। इसलिए, आप सही हैं…यह सीखने और पुनः सीखने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
जी.एच. : रंगमंच और फिल्म, दर्शकों के साथ न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि एक समुदाय के रूप में संवाद स्थापित करने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। यकीनन, रंगमंच कलाकारों और सामने मौजूद दर्शकों से सीधे मुखातिब होता है। एक राजनीतिक कलाकार के रूप में यह आपके प्रदर्शन को क्या लाभ देता है और किस तरह की चुनौतियां पेश करता है?
एस.एस. : इसमें कोई संदेह नहीं है कि रंगमंच में उद्वेलित करने और चीजों को पलट देने की बड़ी ताकत है। एक जीवंत प्रदर्शन (लाइव पर्फॉर्मन्स) के दौरान माहौल एक खास तरह से गरमाता (चार्जड होता) है, उस समय कुछ भी हो सकता है। जो भी होता है, वह एक क्षण में होता है और यही उसकी विशिष्टता है। इसीलिए जीवंत प्रदर्शन से ही पहले ही सेंसरशिप बहुत ही निरर्थक है, महाराष्ट्र में यह अब भी हम पर लागू होता है।
जीवंत प्रदर्शन का चीजों को पलट देने वाला यह गुण अक्सर लोगों को सजग कर देता है और इसके कारण वे अमूमन अति में प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मैं इस अवलोकन का इस्तेमाल एक दूसरा नजरिया प्रस्तुत करने के लिए करना चाहूंगा, यानी कुछ चीजें जिनकी हम कल्पना कर लेते हैं, उन्हें बिना प्रमाण के स्वीकार कर लेते हैं, उन पर सवाल नहीं उठाकर हम अपना ही नुकसान करते हैं।

कोविड महामारी के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण बहस उभर कर सामने आई वह यह थी कि “जीवंतता” के मूल में क्या है। यह बहस तब छिड़ी जब जीवंत प्रदर्शन करने वालों, जैसे कि रंगमंच कलाकार, को डिजिटल की दुनिया में कदम रखना पड़ा और काल्पनिक दर्शकों के लिए प्रस्तुति देनी पड़ी, और वो भी एक पूर्व निर्धारित विजुअल फ्रेम (जो आमतौर पर जूम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) के दायरे में ही देनी पड़ी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह बहुत ही असुविधाजनक था। एक बहुत ही मजबूत शुद्धतावादी रुख था कि डिजिटल डोमेन में प्रस्तुत किया गया थियेटर, थियेटर है ही नहीं। इसके अलावा हमने एक अलग नजारा यह भी देखा कि कितनी तेजी से भारत में रंगमंच से जुड़े लोगों ने जीवंत प्रस्तुति न दे पाने की इस चुनौती से निपटने के लिए कितने नए-नए तरीके खोज डाले। फिर भी जो निराशाजनक था, वह यह था कि जीवंत प्रस्तुति के पूरे विचार को पुनः देखने के अवसर का खो जाना। बहुत सारा जीवंत रंगमंच वास्तव में “मृत” रंगमंच है या फिर घातक थियेटर है, जैसा कि पीटर ब्रुक कहते हैं। एक ऐसा रंगमंच जो बिल्कुल काम नहीं करता है, और किसी के लिए कुछ नहीं करता। और उसकी फिर भी जीवंत प्रस्तुति की जाती है। तो फिर जीवंतता क्या है? और क्या हम वास्तव में पर्याप्त मेहनत करते हैं कि उसे सफल बनाया जा सके? यह समस्या तब आती है जब रंगमंच विशिष्ट रूप से एक बड़े विचार के लिए किया जाता है – उदाहरण के लिए एक्टिविस्ट थियेटर।
जी.एच. : मैंने समुदाय के बारे में बात की है – लेकिन जाहिर है, रंगमंच गृह में मौजूद “अप्रत्याशित समुदाय” आपके आसपास के समुदाय से काफी भिन्न होता है। क्या आपको लगता है कि नुक्कड़ रंगमंच या परंपरागत/लोक रूपों को अपनाने में “जन नाट्य” के रूप में ज्यादा में संभावना है?
एस.एस. : इस प्रश्न में दो पृथक विचार हैं, लेकिन वे आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि संचार में अलग-अलग मंच अलग-अलग संभावनाओं को जगह देते हैं। जो संवाद एक प्रेक्षागृह में और इसके अलावा प्रदर्शन हेतु डिजाइन किए गए स्थान में संभव है, वह शायद “बाहर सड़क पर” करना बहुत ही मुश्किल होगा और यही इसकी उलट प्रस्तुति में भी लागू होता है। दो भिन्न तरह के स्थानों की पहुंच भी अलग है। सड़क (नुक्कड़) ज्यादा लोकतांत्रिक है, वहां कोई भी हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि वहां दर्शक लगातार बदलता रहता है और प्रस्तुति के प्रति प्रतिबद्धता का माप भी अलग-अलग होता है। जब हम “कॉटन 56, पॉलीएस्टर 84” (मुंबई के कपड़ा मिल श्रमिकों के बारे में रामू रामनाथन का नाटक) का प्रदर्शन कर रहे थे, तो श्रमिक दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने की उत्सुकता में हमने छोटे सामुदायिक केंद्रों या फिर खुले में भी काम करने की पेशकश की थी। लेकिन श्रमिकों ने हमें बहुत दृढ़ता से बताया कि वे इस प्रस्तुति को एक औपचारिक सभागार में ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि तभी वे उस अनुभव का आनंद ले पाएंगे।
मैं सोचता हूं कि जब हम नुक्कड़ नाटक के बारे में या फिर “जन” नाट्य के लिए उपयोगी होने के संदर्भ में लोक रूपों को अपनाने की बात करते हैं, इसलिए शायद हम इनका जिक्र करते हैं, इसके अलावा नाटक किस बारे में हैं, तो लोक रूपों में विशेष रंगमंचीय विशेषताएं तो हैं ही। मैंने हमेशा अपने “औपचारिक” काम में इन रंगमंचीय तत्वों में से कुछ को पसंद किया है और उनका मंचन किया है। उदाहरण के लिए, ‘फोर्थ वॉल’, परंपरा को तोड़ने और इस प्रस्तुति में दर्शकों को भी शामिल करना; समय और स्थान में पीछे और आगे जाने की संभावना; और भिन्न तरह की भाषा को दर्ज करने की भी संभावना।
जी.एच. : ठीक जैसे कि कवि बहुत जरूरी होते हैं, हालांकि तर्क दिया जा सकता है कि लिखने के नजरिये से गद्य लिखना आसान है, उसने प्रकाशित करना और बेचना भी आसान है। रिपोर्ताज का काल्पनिक उपयोग करने के साथ डॉक्युमेंट्री फिल्म को लोगों, समय और इतिवृत्त विचारों के लिए बहुत आवश्यक माना जा सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
एस.एस. : अपने प्रश्न में आपके द्वारा एक कवि के विचार का इस्तेमाल करना बहुत ही रोचक है! पिछले कुछ दशकों में डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ है, और इसके द्वारा कुछ बहुत ही सुंदर काव्यकृतियों को भी प्रस्तुत किया गया, जो कि उस समय-काल के लिए एक बहुत ही कीमती इतिवृत्त भी है। कई सारे मायनों में स्वतंत्र डॉक्युमेंट्री फिल्मकारों ने न केवल फिल्म की भाषा को ही आगे बढ़ाया है; बल्कि वे स्वतंत्र विचारों के अंतिम गढ़ रहे हैं जिन्होंने राज्य और मुख्यधारा, दोनों के ही आख्यानों को चुनौती भी दी है और उनका विरोध भी किया है। मैं फिर कहूंगा कि रंगमंच की भांति डॉक्युमेंट्री में भी चीजों को जबरदस्त तरीके से उलट-पलट करने की क्षमता है, जिसके कारण सत्ता अक्सर उन्हें पीछे धकेलती है – जो कि उन बहुत सारे लोगों को, जिन तक वह पहुंचती है, डॉक्युमेंट्री अक्सर अनुपात से बाहर प्रतीत होती है। मुझे याद है कि एक बार हम मुंबई में एक छोटी-सी अनौपचारिक जगह पर एक ऐसी फिल्म दिखा रहे थे जो कि कश्मीर के प्रतिरोध आंदोलन के प्रति काफी सहानुभूति दर्शाती थी। फिल्म को देखने करीब 50-60 लोग आए थे, लेकिन अचानक नजदीकी स्थानीय पुलिस स्टेशन से करीब बीस पुलिसकर्मी वहां आ धमके, उनमें वरिष्ठ इंस्पेक्टर उस स्क्रीनिंग को रोकने के लिए आए थे। यह प्रतिक्रिया पूरी तरह से उस अवसर के लिए अनुपात से बाहर थी, लेकिन मैं समझता हूं कि यह स्वतंत्र विचारों की शक्ति को दर्शाता है।

जी.एच. : एक लेखक, कलाकार या चाहे एक निर्देशक के रूप में, आप विगत को वर्तमान के लिए किस तरह से नए सिरे से अर्थपूर्ण बनाते हैं? और विगत को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने के संदर्भ में बढ़ते उग्र-राष्ट्रवादी आख्यान का प्रतिरोध करते हुए आप इसे किस तरह से करते हैं?
एस.एस. : अतीत और वर्तमान, दोनों को ही लेकर हमारी समझ उनको संदर्भित करने से आती है। ‘सेक्स, मॉरैलिटी और सेंसरशिप’ में हमने अपने समकालीन समय में सेंसरशिप के विचार को समझने के लिए 1972 में राज्य और नागरिक समाज द्वारा नाटक “सखाराम बाईंडर” पर हमले के इतिहास और उसके संदर्भ पर शोध किया। लेकिन पृथ्वीराज कपूर के प्रतिष्ठित नाटक “दीवार” (1945) की दोबारा कल्पना करने के लिए उस समय उस नाटक में दिए जा रहे तर्क को समझने के लिए उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद को लेकर अपनी मौजूदा समझ का इस्तेमाल किया। असहमति के विचार की तलाश वाले “वर्ड्स हेव बीन अटर्ड” में हम समय, स्थान, भूगोल और भाषा के बीच अबाधित रूप से यात्रा करते हैं, ताकि हम इस बात पर पूरा जोर दे सकें कि मानव सभ्यता के लिए असहमति एक अविभाज्य और आवश्यक हिस्सा है। मेरे अनुभव में इस प्रकार की निकटता हमें एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही शिक्षाप्रद अर्थ की ओर ले जाती है।
कृष्ण सिंह द्वारा हिंदी में अनुवादित। अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ें।