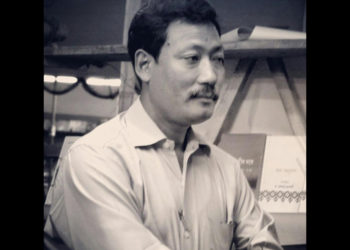उत्तराखंड का बचवाली।
पूर्वी उत्तरप्रदेश का नोमा।
दक्षिण भारत का देवपुर।
ये वो जगहें हैं जिन्हें अपने देश के भूगोल में मैं शायद ही कभी ढूँढ़ पाऊँ–कुछ तो घुमक्कड़ी के साथ अपने असहज रिश्ते के कारण और कुछ इस कारण कि ठीक-ठीक ये नाम-पते शायद इस भूगोल में कहीं हैं ही नहीं।
पर उस कथादेश के भूगोल में ये जगहें हैं जो मेरा देखा-जाना और घूमा-छाना हुआ है। मैं आपको इनके पते बता सकता हूँ| बचवाली का पता है, राकेश तिवारी का उपन्यास फसक (2017)। नोमा–चंदन पाण्डेय का वैधानिक गल्प (2020)। देवपुर–गीता हरिहरन का आइ हैव बिकम द टाइड (2019)।
इन सबकी अपनी-अपनी पहचान है। इन जगहों पर भटकते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उसी-उसी जगह दुबारा-तिबारा पहुँचा हूँ।
पर इनमें एक गहरी समानता भी है, और वही इन्हें एक साथ याद करने की वजह है। इन सभी नगरों-क़स्बों में ‘अच्छे दिन’ टूटकर आए हैं और ‘नया भारत’ शान से बजबजा रहा है।
बचवाली में अंधविश्वास और वक़रियानूसी की वापसी ‘अच्छे दिन’ की पहचान है। फेसबुक और व्हाटसैप से लैस स्मार्ट फ़ोन नामक यंत्र का लोकप्रिय होना और तर्क-विवेक की ओर बढ़ते रुझान का बीच रास्ते ही पीछे की ओर मुड़ जाना यहाँ लगभग युगपत प्रक्रियाएं हैं। खूब पढ़नेवाले और तर्क-विवेक को ही एकमात्र कसौटी माननेवाले पी थी (प्रेम प्रकाश पंत) जैसे लोग बहुत लोकप्रिय तो पहले भी नहीं थे, पर कम-से-कम उनकी विचित्रता के प्रति, थोड़ी दूरी बरतते हुए ही सही, एक तरह का सम्मान था। अब स्थिति यह है कि लोग उन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। असंगत बातों पर सीधा तंज़ कसने वाला लाल बुझक्कड़ तो अक्सर हिंसा का शिकार होता है। ऐसे सभी लोग अब ‘पगलैट’ की श्रेणी में आ गए हैं। नायक तेजू पगलैट भले न माना जाता हो, अविवेकी हिंसक भीड़ का विरोध करने के बाद उसके घर पर भी रात गए पत्थर बरसाए जाते हैं।
गोया ‘वक़्त के एक अँधेरे दौर से गुज़र चुकने के बाद लोग फिर से अँधेरे के तिलिस्म मे फेस रहे हैं। अंधकार का काला गुबार। स्वागत में बिछे लोग। ऐसे कहीं समय को लौटना चाहिए?’
‘फसक (गप्प) की परंपरा के लिए विख्यात बचवाली में भ्रमण करते हुए आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में वहाँ फसक की प्रकृति आमूलतः बदल गई है। पहले वह समय काटने के काम आती थी। मनोरंजन के अलावा वह कई बार निंदारस के लिए भी इस्तेमाल होती थी जो बाज़ दफ़ा व्यक्तिगत मान-अपमान तक भी जा सकता था। पर उसके पीछे कभी सामूहिक या सामुदायिक अपमान की भावना नहीं रही और भले ही उससे कोई लोक-हित न सधता रहा हो, कम-से-कम लोक का अहित नहीं होता था। 204 आते-आते इसमें बुनियादी बदलाव आ गया।
‘कई फसकें तो अब बनी-बनाई आने लगी हैं। कभी-कभी पुर्ज़े बाहर से आते हैं और स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से ‘फसक को असेम्बल कर लिया जाता है। इसमें लद्धड़ और फर्राठा, दोनों क्रिस्म के लोग समान रुचि ले रहे हैं। लड्ड़ों के बीच यह मौखिक रूप से फैलती है। मानो ये श्रुति परंपरा के वाहक हैं| चुस्त लोगों के बीच फसक स्क्रीन पर लिखी और पोस्ट की जाती है। इससे एक क्षण में यह दूर-दूर तक पहुँच जाती है। नई फसक में परंपरागत फसक से काफ़ी अंतर है। पुरानी फसक में सच भी थोड़ा-थोड़ा संदेहास्पद लगता था। पर उसकी रोचकता ही उसकी लोकप्रियता थी। नई फसक में संदेहास्पद चीज़ें भी भरोसेमंद हो गई हैं। क्योंकि इसमें आस्था का तत्त्व है। वह किसी सवाल, संदेह और चुनौती से परे है।… नयी फसक में कुछ नायक होते हैं और कुछ खलनायक। खलनायक हमेशा माथे पर गूम (गूमड़) निकाले हुए डरावने लोग होते हैं। धोखेबाज़ और ग़ैर-भरोसेमंद| जबकि नायक सर्वशक्तिमान, सर्वगुणसम्पन्न, सर्वहितकारी, सच्चे और सबसे अच्छे। उजले और टीका लगे ललाट वाले।’
फसक की प्रकृति का यह बदलाव एक गहरी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसकी कमान भय्याजी, चंदू पांडे जैसे राजनीतिज्ञों और चुन्नी महराज जैसे ढोंगी बाबा के हाथ में है। इलाक़े के ढाई-तीन सौ युवकों को भय्याजी का मासिक वज़ीफ़ा मिलता है, जिसका मतलब है, हर महीने तीन-तीन सौ रुपये का रीचार्ज कूपन। गौ-कथा के आयोजनों को अपने भीतर मन से एक नया टंटा मानने वाले भय्याजी अब छोटे-छोटे ब्रतों-त्योहारों के सार्वजनीकरण में एक नई राजनीतिक संभावना देखकर यह भाषण देने लगे हैं कि ‘जब तक कोई धार्मिक आयोजन अपनों के अंदर अपार श्रद्धा का और दूसरों के भीतर भय का संचार न करे, तब तक उसकी सफलता पर संदेह करना चाहिए|… अपने अपने बिलों में घुसकर चुपचाप पूजा करने से क्या लाभ? पूजा को सार्वजनिक अनुष्ठान में बदलना होगा।’ आधुनिक शिक्षा के प्रति नन्नू महराज की वितृष्णा को प्रतिध्वनित करते हुए वे कहते हैं, ‘अगर बच्चे बहकी-बहकी बातें करने लगे हैं तो समझ लेना चाहिए कि वे ग़लत राह पर चल पड़े हैं। कोई उन्हें बरगला रहा है। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लाल झंडे के गढ़ों में कतई नहीं भेजना चाहिए।’
बलात्कारी बाबा नन्नू महराज, चंदू पांडे को भी राजनीतिक गुरुमंत्र देने का काम करता है। पढ़े-लिखे लोगों की तार्किक बातों के आगे जिस चंदू के पैर उखड़ जाते हैं, उसे इस मंत्र से बड़ी मदद मिलती है कि ‘बदतमीज़ी ज़बान को लकवाग्रस्त कर देने का अचूक हथियार है।’ बाबा का निर्देश है, ‘हूट करो… ऐसे चिललाने लगो कि सामनेवाले की बात दब जाए। ऐसा कड़ा विरोध करो कि दुबारा बोल न पाए। दूसरों को बोलने की आज़ादी उतनी ही देनी चाहिए जितना उचित है।’
इस बचवाली में घूमते हुए आपको संदेह नहीं रह जाता कि यह अपनी विशिष्ट पहचान खोए बगैर आज के भारत का माइक्रोकॉस्म बन गया है, पिंड में ब्रह्मांड सरीखा। लेखक कई जगह इस क़स्बे का नाम भी ऐसे लेता है जैसे भारत कहना था, बचवाली कह गए लालबुझक्कड़ से जुड़ा एक प्रसंग है:
‘एक दिन उसने यूँ ही हवा से कह दिया, “बचवाली की गाँड़ के नीचे ज्वालामुखी सुलगाने की तैयारी चल रही है।”
किसी ने उसका गला पकड़ लिया, “किस बारे में बात कर रहा है बे?”
“पाकिस्तान के बारे में। ग़लती से मुँह से बचवाली निकल गया।” दो बार पहले पिट चुके लालू का उत्तर था।’
यह उपन्यासकार का कौशल है कि लालबुझक्कड़ जैसे ही बचवाली को ‘पाकिस्तान’ से प्रतिस्थापित/रिप्लेस करता है, आप बचवाली में हिंदुस्तान की ध्वनि सुन लेते हैं। यह ध्वनि पूरे उपन्यास में अनुगूंजित है और उपन्यासकार यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे अनसुना न कर पाएं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ख़बर बनने वाली घटनाएं भी बीच-बीच में बचवाली की घटना बनकर आती हैं।
‘…एक अध्यापक के भाषण से केहड़ेन (माँस के जलने की दुर्गंध) आने की सुगबुगाहट क़िस्से में तब्दील हो रही थी। एक नाटूय-मंडली के सदस्यों को कॉस्ट्यूम में दौड़ाये जाने की वीर-गाथा ऐसे सुनाई जा रही थी जैसे वीर-रस की कविता हो’
यह किसी हद तक आश्चर्य का ही विषय कहा जाएगा–ज़ाहिर है, सुखद आश्चर्य का, चित्रित यथार्थ जितना भी दुखद हो–कि ‘अच्छे दिन’ वाली सरकार के आने के तीन सालों के भीतर हिन्दी में यह उपन्यास आ चुका था।
नोमा नामक क़स्बा, जिसका पता चंदन पाण्डेय का वैधानिक गल्प है, इस मायने में काफ़ी अलग है कि उसे लघु भारत बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। वह माइक्रोकॉस्म के बजाए नए भारत का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। यहाँ स्थानीय कॉलेज में पढ़ाने वाला और अपने विद्यार्थियों-साथियों के साथ एक नाट्य-मंडली चलाने वाला रफ़ीक़ कुछ दिनों से ग़ायब है। उसकी पत्नी अनुसूया, जो वाचक की भूतपूर्व प्रेमिका है, एफ़आईआर दर्ज कराने में नाकाम रहने के बाद दूर गुड़गाँव में रहने वाले वाचक से मदद की गुहार लगाती है और आप उसी प्रथम पुरुष वाचक के साथ गोरखपुर से सत्तर किलोमीटर दूर नोमा पहुंचते हैं। धीरे-धीरे आपके सामने एक भयावह कहानी खुलनी शुरू होती है, जिसका बस काम भर खुलना उसकी भयावहता को और बढ़ा देता है। कहानी यह है कि रफ़ीक़ की मंडली ने पुलिस महक़मे से निलंबित एक सब-इन्स्पेक्टर अमनदीप सिंह की सच्ची कहानी को केंद्र में रखकर नुक्कड़ नाटक तैयार किया था जिसके दो-एक प्रदर्शन हो चुके थे। अमनदीप सिंह की ग़लती यह थी कि उसने एक हिन्दू लड़की से प्यार करने वाले नियाज़ को हिंसक सांप्रदायिक भीड़ से बचाया था। उसे वित्तीय अनियमितता के नाम पर मुअत्तल किया गया। इस सच्चाई को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक ले जाने की कोशिश में रफ़ीक़ की मंडली को भी सांप्रदायिक तत्त्वों के हमले का निशाना बनना पड़ा। पर वे अपने काम को आगे जारी रखने पर बज़िद रहे। क़स्बे के प्रसिद्ध दोल मेले में भी इस नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन की तैयारी उन्होंने कर रखी थी। उससे ठीक पहले रफ़ीक़ ग़ायब हो गया। फिर उसकी मंडली की एक सदस्या, रफ़ीक़ की छात्रा ग़ायब हो गई। कहानी जिस तरह आपके सामने खुलती है, उससे आपको धीरे-धीरे समझ में आता है कि वे एक योजना के तहत ग़ायब किए गए हैं| इससे स्थानीय राजनीति, पुलिस प्रशासन और कॉलेज के प्रबंधन पर मज़बूत शिकंजा जमाए हुए सांप्रदायिक तत्त्वों को यह क़िस्सा गढ़ने में आसानी हो गई है कि रफ़ीक़ सुनियोजित तरीक़े से लव-जेहाद में लगा एक अभ्यस्त मुजरिम है, जिसने पहले एक हिन्दू लड़की से विवाह करके उसे हरियाणा से भगाकर इतनी दूर पूर्वी उत्तरप्रदेश में ला पटका और अब फिर अपनी एक हिन्दू छात्रा को फँसाकर भगा ले गया है। आपके नोमा पहुँचने का बाद इस तरह की खबरें मुख्तलिफ़ माध्यमों से आप तक पहुँचती रहती हैं| ब्हाटसैप पर घूमता एक वीडिओ क्लिप भी आप देखते हैं जिसमें रफ़ीक़ अपनी उस छात्रा से प्रेमालाप कर रहा है। बाद में आपको पता चलता है कि यह उनके उसी नाटक के रिहर्सल की वीडिओ से निकाला हुआ हिस्सा है, जिसे नाटक नहीं, एक सच की तरह लव-जेहाद के प्रमाण के तौर पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जा चुका है। आपके नोमा पहुँचने के बाद नाटक-मंडली के दो और सदस्य बारी-बारी से ग़ायब होते हैं। गोया एक डरावने अँधेरे में हाथ मारते हुए कथा आगे बढ़ती है और उपन्यास उस मुक़ाम पर लगभग एक झटके के साथ समाप्त होता है जहाँ सारे उलझे हुए धागे वाचक के सामने, और इस तरह आपके सामने, इस बिन्दु पर आकर सुलझ जाते हैं कि लिंचक भीड़ से मुस्लिम युवक को बचाने वाले अमनदीप को केंद्र में रखकर तैयार किया गया नाटक न होता तो ग़ायब होने/किए जाने का यह रहस्यमय सिलसिला भी न होता, जिसकी सुध लेने को पुलिस और नगर प्रशासन न सिर्फ़ राज़ी नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण और अग्र-सक्रिय भागीदारी के साथ ही जिसे अंजाम दिया जा रहा है।
राज्य-तंत्र पर क़ाबिज़ हिंदुत्ववादी फ़ासिस्टों की कार्यविधि को खोलता यह छोटा-सा उपन्यास एक से दो बैठकों में खुद को पूरा पढ़वा ले जाता है। रहस्यमय स्थितियों के बीच से असलियत के धीरे-धीरे उद्घधाटित होने का शिल्प इसे दिलचस्प तो बनाता ही है, खबरों के साथ हमारे रिश्ते का एक अंतर्दृष्टिपूर्ण और प्रबोधनकारी मॉडेल भी निर्मित करता है। यहाँ हम जिस जगह से झूठ और अफवाह को सच का स्थानापन्न बनाने की फ़ासिस्ट कार्यविधि को बेपर्द होता देखते हैं, वह खबरों के पाठक-दर्शक-श्रोता की जगह है। यह ‘वेंटेज पॉइंट’ इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसी अवस्थिति से जनता के सबसे बड़े हिस्से को सच की शिनाख्त करनी है। यह माध्यमों से घिरे हुए एक पाठक की निगाह में प्रभुत्वशाली नेरेटिव की वैधता को अस्थिर कर देने, संदिग्ध बना देने और एक अवगुंठन का वर्जा दे देने की कला है। कहने की ज़रूरत नहीं कि इस उपन्यास से गुज़रे हुए पाठक के लिए 29 अगस्त 2020 के अखबारों में छपी उस खबर के मायने बहुत अलग होंगे जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के गृह विभाग को ‘लव जेहाद’ की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेने, उन्हें रोकने की रणनीति तैयार करने और ज़रूरत हो तो नए क़ानून बनाने की हिदायत दी है! साथ में राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव का यह बयान भी छपा है कि लव जेहाद के इन ‘आरोपितों के खिलाफ़ कार्रवाई की ज़रूरत है और हमें निष्ठुर होना होगा। इन दिनों सोशल मीडिया हर जगह मौजूद है और ऐसी चीज़ें दूसरों के दिमाग़ पर भी असर डालती हैं’ (29 अगस्त, द इंडियन एक्सप्रेस, पृष्ठ 8)| यही सरकारी तंत्र द्वारा पेश किया गया बैधानिक गल्प है।
कितने नियाज़ और रफ़ीक़ इस गल्प के निशाने पर हैं, कितनी त्रासदियाँ क़ानून और व्यवस्था के दिखावे की इस आड़ में पल रही हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है, जिसकी दिशा में नोमा का वृत्तान्त हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है।
नोमा के बाद, आइए, दक्षिण भारत चलते हैं। देवपुर। यहीं वह विश्वविद्यालय है जहाँ प्रो. पी एस कृष्णा पढ़ाते हैं। नहीं, पढ़ाते थे। विश्वविद्यालय परिसर में ही उन्हें बाइक पर सवार दो युवकों ने गोली मार दी। दोनों युवक हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के लिए कृतसंकल्प एक संस्था से जुड़े हुए थे और इसमें बाधा बननेवाले हर ‘राक्षस’ का ‘वध’ करना उनका परम कर्तव्य था। पर ठहरिए, यह ‘वध’ देवपुर में आपके पहुँचने के लगभग 300 पृष्ठों के बाद होगा। तब तक के लिए तो प्रो. कृष्णा के बारे में यही कहना ठीक होगा कि वे पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाना, उनका व्याख्यान देना और प्रचलित धारणाओं को अपने व्यवस्थित शोध के आधार पर चुनौती देना गुरु (श्री श्री श्री) संतोष, हिन्दू राष्ट्र सभा और देवपुर हिन्दू सेने आदि को सख्त नापसंद है। उनके एक बहुचर्चित व्याख्यान के बाव:
‘गुरु (श्री श्री श्री) संतोष ऐसी मनःस्थिति में है जिसमें क्रोध और उत्तेजना बराबर-बराबर मात्रा में हैं। कृष्णा के खिलाफ़ अभियोग स्पष्ट हैं| इस तथाकथित प्रोफेसर ने कननदेव के द्वारा जल-समाधि के गौरवपूर्ण चुनाव को आत्महत्या बताया है। यह तो फिर भी कमतर अपराध है, उन बातों के मुक़ाबले जो कृष्णा कथित रूप से अपने द्वारा पाए गए भोजप्रों के बारे में कहता है। कृष्णा ने बेशर्मी से यह दावा किया है कि कन्नदेव अपने आरंभिक जीवन में कन्नप्पा पुकारे जाते थे, और वे एक धोबी के बेटे थे जिसका पिता मवेशियों की खाल उतारने का काम करता था। संतोष के पेट में मरोड़-सी उठती है। क्या कोई अंत नहीं है संतों के जीवन के विरूपण का? हिन्दू इतिहास के विरूपण का? इन हिन्दू-द्रोहियों का यह घमंड! निश्चय ही, पादरी और मुल्ले तो गौरवशाली हिन्दू राष्ट्र की दिशा में हमारे प्रयाण को बाधित करने के लिए कुछ भी करेंगे। वह तो जानी हुई बात है। लेकिन ये घर के चूहे, हिन्दू समाज के अंदर के चूहे तो सबसे गए-गुज़रे हैं। इस आदमी का नाम कृष्णा है। यह महाभारत जैसे महाकाव्य का अध्यापन करता है–प्रज्ञा का वह पुंज जिसमें भगवद गीता रूपी समुज्ज्वल आत्मा है। क्या इसे इस तरह की गंदगी फैलाते लज्जा नहीं आती? अपने ही घर के सबसे पवित्र कक्ष में मल- विसर्जन? […] यह एक खुली चुनौती है। यह एक मिसाल क़ायम करने का अवसर भी है। गद्दारों से, राक्षसों की तरह ही, समुचित रीति से निपटने की ज़रूरत है।’ (अनुवाद हमारा)
तो प्रो. कृष्णा का अपराध यह है कि वे हिन्दू इतिहास को और हिन्दू संतों के जीवन को तोड़ने-मरोड़ने की साज़िश में लिप्त हैं! असल बात यह है कि हिन्दू राष्ट्र बनने के लिए तैयार होते भारत में मध्यकालीन भक्त कवि कननदेव को हिन्दुत्व के एक आइकॉन के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। उनका वास्तविक इतिहास मिटाया जा चुका है। इस तथ्य पर मिट्टी डाली जा चुकी है कि वे पशुओं का चमड़ा उतारने वाले एक दलित के पौत्र थे, जिनके लिए पढ़ना-लिखना सिर्फ़ इसलिए संभव हो पाया कि जात-पाँत को खत्म करने में लगा एक मुक्तिकामी आंदोलन ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देता उठ खड़ा हुआ था। उसकी दबी-छिपी झलक प्रो. कृष्णा को कननदेव की कविताओं मे मिलती है और वे उस दिशा में अपने शोध को आगे बढ़ाते हैं, जिसका निष्कर्ष यह है कि उन्होंने जल-समाधि नहीं ली थी बल्कि भेदभाव का विरोध करने वाली मुहिम के वर्चस्वशाली शक्तियों द्वारा नेस्तनाबूब कर दिए जाने के बाद हताशा में खुदकुशी की थी।
ऐसे शोध-निष्कर्षों पर पहुँचने वाले और उन्हें भाषणों-लेखों के जरिए प्रसारित करने वाले विद्वान से ‘समुचित रीति से निपटना’ तो बनता है! सो बाक़ायदा इस राक्षस के नाश के लिए एक भूमिगत संगठन–इसमें आप सनातन संस्था की झलक देख सकते हैं–के दो युवकों को तैयार किया जाता है। इस संगठन के पास एक पूरी फ़ेहरिस्त है जिसमें प्रो. कृष्णा पाँचवें नंबर पर हैं। उस फ़ेहरिस्त में वे शख््सियतें हैं जो, संस्था के डॉ. राजेश के शब्दों में, ‘हार्डकोर एंटी-हिन्दू हैं। वे ऐक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट हैं; यहाँ तक कि, कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ, कवि और संगीतकार, अध्यापक और प्रोफेसर हैं।’
कार्यभार निश्चित होने और 7.65 एमएम की पिस्तौल मिलने के बाद दोनों युवक देवपुर जाकर कुछ दिन रहते हैं, प्रो. कृष्णा की दिनचर्या का अध्ययन करते हैं और फिर सबसे उपयुक्त अवसर चुनकर प्रोफेसर के कपाल के बीचोंबीच अचूक निशाना लगाते हैं।
अगर सिर्फ़ प्रो. कलबुर्गी की हत्या की याद दिलाने वाला यही प्रकरण उपन्यास में होता, तब भी अपने ब्योरों की बारीकी के कारण यह पठनीय होता, पर यहाँ दो और कथाएं समानांतर चलती हैं, जिन्होंने प्रो. कृष्ण की कथा के साथ मिलकर उपन्यास के अर्थ को बहुत व्यापक फलक दे दिया है। एक कथा आठ सदी पहले के चिक्का/चिक्कइया और उसके बेटे कन्नप्पा/कन्नदेव की है, जिसमें एक असाधारण जाति-विरोधी आंदोलन का उत्थान और पतन चित्रित है—किस तरह एक सपना आकार लेता है और कुछ समय तक अपने बने रहने का संघर्ष करते हुए अंततः प्रतिक्रियावादी उच्च जातियों के निर्णायक हमले की भेंट चढ़ जाता है, इसका चित्रण। दूसरी कहानी तीन दलित युवाओं की है—दो युवक और एक युवती। वे अपनी पढ़ाई के दौरान किस तरह के अपमान और उत्पीड़न से गुज़रते हैं, किस तरह वे बाहर भी और अपने भीतर भी उससे लड़ते हैं, इसके मार्मिक ब्योरों से उनकी कहानी बुनी गई है। अंततः उनमें से मेडिकल में दाखिला लेने वाला सबसे ज़हीन युवक, सत्य, खुदकुशी करता है। इन युवाओं की कहानी का प्रकटतः उपन्यास की दूसरी समानांतर कथाओं से बहुत क्षीण-सा संबंध है—बस इतना ही कि प्रो. कृष्णा के कन्नदेव संबंधी काम से उन्हें दलित इतिहास को समझने में थोड़ी मदद मिलती है और उनकी हत्या के बाद इन तीनों में से खुदकुशी न करने वाले दो युवा, रवि और आशा, विराट विरोध-प्रदर्शनों का हिस्सा बनते हैं—पर अंतर्वस्तु की दृष्टि से इनका संबंध बहुत गहरा है। चिक्कइया और कन्नप्पा की कहानी के समानांतर चलती तीन दलित युवाओं की कहानी बताती है कि इन आठ सौ सालों में क्या बदला है और क्या नहीं बदला, और यह भी कि वो क्या चीज है जिसने एक सच्चे इतिहास की खोज करने वाले विद्वान को हिन्दू राष्ट्र- वादियों के निशाने पर ला विया। उपन्यास में चित्रित हिन्दू धर्म सभा और देवपुर हिन्दू सेने जैसी संस्थाएं दलित मुक्ति की आज की परियोजना के साथ वही कर रही हैं जो ब्राह्मणवादियों ने आठ सौ साल पहले जाति-उच्छेदक मुहिम के साथ किया था और जिससे हताश होकर कन््नदेव को आत्महत्या करनी पड़ी थी।
आइ हैव बिकम द टाइड एक स्तर पर तीन हत्याओं की कहानी है, जिनमें से दो को हम सतही तौर पर आत्महत्या कह सकते हैं। जिन शक्तियों ने प्रो. कृष्णा को मारा, वे ही कन्नप्पा/कन्नदेव और सत्य के भी हत्यारे हैं—इस बात को तर्क से आगे अहसास तक हमारे भीतर उतारना इस उपन्यास को बड़ा बनाता है। मेरे पढ़े हुए उपन्यासों में से यह अकेला है जिसने हिन्दुत्व के मौजूदा उभार को मुस्लिम-विरोधी घृणा की जगह दलित-विरोधी घृणा और जाति-तंत्र के संरक्षण के साथ जोड़कर न सिर्फ़ देखा है बल्कि बहुत तैयारी के साथ अपना केन्द्रीय कथ्य बनाया है। यह उपन्यास गोया कहना चाहता है कि भारतीय समाज में जब-जब जाति के उत्पीड़नकारी श्रेणी-क्रम के खिलाफ़ कोई व्यवस्थित और मज़बूत आंदोलन खड़ा हुआ है, तब-तब यथास्थितिवादी शक्तियों ने नयी तैयारी के साथ उसका मूलोच्छेद करने का बीड़ा उठाया है और हिन्दुत्व का मौजूदा उभार भी उसी की एक कड़ी है। यह, वस्तुतः, जातियों के श्रेणी-क्रम का उन्मूलन करने में सन्नद्ध भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित भारत के खिलाफ़ है।
बचवाली, नोमा और देवपुर की ये कहानियाँ आज के भारत के अवैधानिक गल्प हैं, जो आपको इतना कल्पनाक्षम बनाते हैं कि खबरों में आने वाली घटनाएं आपके लिए सजीव हो जाती हैं। आप घटनाओं को समाचार की निर्जीव देह से निकालकर जीवंत विवरणों में घटित होता हुआ देखने लगते हैं। क्या आश्चर्य कि इन्हें पढ़ते हुए वे दो मामले मेरे ज़ेहन में कौंधते रहे जिनकी ओर इनमें कोई संकेत नहीं है (हो ही नहीं सकता था, ये बाद के मामले हैं)—दिल्ली दंगे और भीमा कोरेगाँव! शायद वे इस बात की तसदीक़ कर रहे थे कि जिस समय वैधानिक गल्पों से माध्यम पटे पड़े हैं, ऐसे अवैधानिक गल्पों की कितनी ज़रूरत है। अलबत्ता, यह नहीं भूलना चाहिए कि रचनाओं की महत्ता का आधार विषय नहीं होता, वस्तु और उसकी प्रस्तुति होती है। ये तीन उपन्यास अपने विषय की समानता के कारण यहाँ साथ भले ही रखे गए हों, इनके महत्त्व का कारण वह नहीं है। इसी विषय पर कोई बहुत कमतर गुणवत्ता वाला उपन्यास लिखा जाना बिल्कुल संभव है और मेरी खुशक़रिस्मती है कि ऐसी किसी रचना से मेरा पाला नहीं पड़ा।
Read the English translation by Salim Yusufji here.