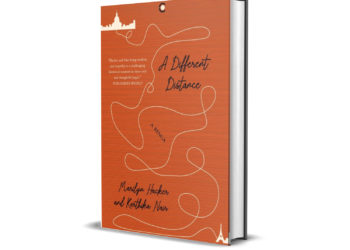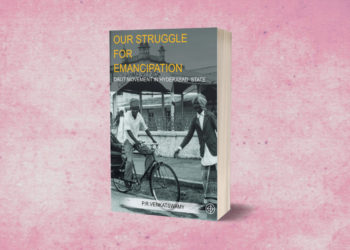जाने-माने इतिहासकार एस. इरफ़ान हबीब की किताब भारतीय राष्ट्रवाद : एक अनिवार्य पाठ (संपा) (राजकमल प्रकाशन, 2023) आज के समय में राष्ट्रवाद को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान में जिस राष्ट्रवाद का हो-हल्ला मचाया जा रहा है वह उस समावेशी राष्ट्रवाद से एकदम उलट है जिसकी परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों-नायिकाओं ने की थी। जैसा कि इतिहासकार इरफ़ान हबीब कहते हैं, “हमारे राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति की हमारी अवधारणा को उन पुरुषों और स्त्रियों के प्रामाणिक लेखन के आईने में समझा जा सकता है जिन्होंने हमारे लिए उसे परिभाषित किया। इनमें से कई लोग राजनीतिक चिन्तक और नेता थे, कई आन्दोलनकारी भी थे जो दिन-रात उपनिवेश विरोधी संघर्षों में लगे हुए थे। भारतीय राष्ट्र, राष्ट्रवाद और संस्कृति की अवधारणा में वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक आन्दोलनकारियों ने भी अपना योगदान दिया। राष्ट्रवाद और संस्कृति के तत्वों से मिला-जुला यह योगदान दरअसल एक उदार-मध्यमार्गी राष्ट्रवाद की परिकल्पना करता था जो कालान्तर में धीरे-धीरे एक ऐसे चरण में पहुँच में गया जहाँ केन्द्र में धर्म आ गया। फिर कई अन्य चरणों से होता हुआ यह अन्तत: आम सहमति आधारित एक समावेशी राष्ट्रवाद में परिणत हुआ।”
इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद और उसके विकास क्रम को समझने के लिए हम महादेव गोविन्द रानाडे, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल, श्री अरबिन्दो, अल्लामा इक़बाल, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, प्रफुल्ल चन्द्र राय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. आंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी, सुभाषचन्द्र बोस, भगत सिंह, एम.एन. रॉय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खान, ख़्वाजा अहमद अब्बास और जयप्रकाश नारायण के विचारों से रू-ब-रू होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हुए भारतीय समाज पर आज जिस इकहरे राष्ट्रवाद को थोपा जा रहा है वह भारत के समावेशी मूल्यों को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। जैसा कि इरफ़ान हबीब लिखते हैं, “गांधी, नेहरू, आंबेडकर, पटेल, आज़ाद और अन्य ने भारतीय राष्ट्रीयता के विचार को स्पष्टता के साथ रेखांकित करते हुए उसके चार स्तम्भों के रूप में जनतंत्र, बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को स्थापित किया। इन बरसों में ये चारों खम्भे कमज़ोर हुए हैं और अब वे ढहने की कगार पर हैं। चुनाव में किसी एक की जीत और दूसरे की हार से यह नतीजा नहीं निकाल लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्रवाद के असल मूल्य अप्रासंगिक हो गए हैं।”
इतिहासकार इरफ़ान हबीब ने इस पुस्तक में 42 पेज की भूमिका लिखी है। इसी भूमिका से कुछ अंश हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

आज भारत में राष्ट्रवाद और संस्कृति की अवधारणा का जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है वह विकृत है। अब यह राष्ट्र या संस्कृति के बारे में गंभीर चिन्तन का मामला नहीं है बल्कि एक लोकप्रिय बहुसंख्यकवादी अलगाववाद द्वारा उछाला गया एक नारा-भर है। हुआ यह है कि इतने वर्षों में राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में जो ताक़तवर तबक़ा हाशिये पर पड़ा रहा था, वह अचानक मुख्यधारा के केन्द्र में आ गया है। राष्ट्रवादी मुहावरेवाज़ी हमेशा से लोगों का ध्रुवीकरण करने में एक उपयोगी औज़ार साबित हुई है। यह दुनिया-भर में कारगर रही है और विनाशक परिणामों के साथ अक्सर इसका इस्तेमाल किया गया है। लोगों की आदिम प्रवृत्तियों को अपील करके जगाने वाली यह राजनीति व्लादिमीर पुतिन से लेकर शिंजो आबे, एरगोदन, डोनाल्ड ट्रम्प और नरेन्द्र मोदी तक दुनिया-भर में समान रूप से देखी जा सकती है। इन सबने जनता को ‘अन्य’ का भय दिखाकर सफलतापूर्वक बाँटा है। इनके नारे में ‘अन्य’ को देश के दुश्मन, संस्कृति के दुश्मन और राष्ट्र के विकास, यहाँ तक कि उसके वजूद को ख़तरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज हमारे राष्ट्रवाद को लगातार एक शत्रु की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी चीज़ जिससे नफ़रत की जा सके। यह राष्ट्रवाद एकरूपता की मांग करता है, किसी भी विचलन को पसन्द नहीं करता बल्कि यह कहें कि राष्ट्रवाद की अपनी प्रस्थापना पर सवाल उठाए जाने से ही नफ़रत करता है। यह संस्कृतियों, विचारों, खाने-पीने की तरीके, पहनने-ओढ़ने के तरीक़े और यहाँ तक कि मनोरंजन के अलग-अलग साधनों में विविधता को भी पसन्द नहीं करता है। आज राज्य द्वारा संरक्षित यह सनकी राष्ट्रवाद हमारे नागरिकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ख़तरनाक हथियार है। एरिक हॉब्सबॉम ने इस झंडाधारी राष्ट्रवाद को बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में यूरोप में उभरते हुए देख लिया था, जहाँ विदेशियों के ख़िलाफ़ देश का झंडा लहराया जाता था। उन्होंने पाया कि हर क़िस्म के राष्ट्रवाद का आधार दरअसल एक ही है : जनता द्वारा अपने राष्ट्र के प्रति भावनात्मक स्तर पर पहचाने जाने की स्वीकार्यता और राजनीति, ख़ासकर चुनावों का जनतांत्रिकरण, जो लोगों को इस भावना के इर्द-गिर्द एकजुट करने के पर्याप्त मौक़े देता था। आज हम भारत में जिस परिघटना से गुज़र रहे हैं, हॉब्सबॉम ने उसे ही स्वर देते हुए कहा था कि जब राज्य इस क़िस्म के राष्ट्रवाद को भड़काकर लोगों को इकट्ठा करते हैं तो वे उसे ‘देशभक्ति’ का नाम देते हैं। पहले से स्थापित राष्ट्र-राज्यों में उभरे मूल ‘दक्षिणपंथी’ राष्ट्रवाद का अन्तिम लक्ष्य देशभक्ति पर अपना एकछत्र दावा करना था और इस तरह बाक़ी हर किसी को किसी-न-किसी क़िस्म का देशद्रोही ठहरा देना था। राष्ट्रवाद को दरअसल एक धर्मशास्त्र में बदला जा रहा था जहाँ उसकी आलोचना करना धर्मविरोधी था, कुफ़्र था। आज भी ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद को एक पवित्र और पूजनीय स्वरूप देकर खुलेआम अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़तरा पैदा कर रहे हैं। हाल ही में शिव विश्वनाथन ने कहा था कि ‘स्वाधीनता आन्दोलन के राष्ट्रवाद से – जो विचारों का एक बहुरंगी समुच्चय था – राष्ट्र की एकरूपता तक का संक्रमण अब पूरा हो चुका है।’
लेकिन यह संक्रमण अचानक नहीं हुआ। इसके बीज आज़ादी के पहले ही बो दिए गए थे जब आज़ादी का संघर्ष अपने उरूज़ पर था। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें अपने स्वतंत्रता संघर्ष से जो विरासत मिली उसने धर्म, भाषा, जाति, वर्ग और यहाँ तक कि क्षेत्र से भी ऊपर उठकर जाते समावेशी तरीक़े से हमारे राष्ट्रवाद और संस्कृति को परिभाषित किया। उसे बेशक उन हिन्दुओं और मुसलमानों से चुनौती मिली जो अलग-अलग पहचानों के इर्द-गिर्द भारतीयों को बाँटने के प्रति कटिबद्ध थे। बीसवीं सदी की शुरुआत से ही दो तरह के समूहों के बीच संघर्ष चल रहा था। एक वे जो भारत की अनेकता में एकता की तलाश करने में जुटे थे और दूसरे वे जो भारत को अलग-अलग राष्ट्रों में बाँटने में जुटे थे। मौजूदा दौर में राष्ट्रवाद की चादर में बड़ी चालाकी से लपेटे गए बहुसंख्यकवादी राजनीतिक व सांस्कृतिक उभार को समझने के लिए हमें 1920 से 1940 के दशक के बीच के दौर को देखना होगा जब समावेशी विरासत को अपने शुरुआती निर्माणकाल से ही इन ताक़तों से चुनौती शुरू हो गई थी।
[…]
आज की दक्षिणपंथी ताक़तें, जो अक्सर ख़ुद को राष्ट्रवादी आवरण में पेश करती हैं, इन्होंने राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं लिया। इनसे जब इनके अतीत के बारे में सवाल किया जाता है तो ये भागकर अपने सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यभारों में छुप जाते हैं जिनमें ये लगे हुए थे और बड़ी आसानी से इस बात की उपेक्षा कर देते हैं कि बाक़ी कितनों ने उस दौरान औपनिवेशिक राज के हाथों उत्पीड़न झेला और बलिदान दिया। हाल ही में नेहरू स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय में लगी एक प्रदर्शनी पर मेरा ध्यान गया जहाँ दक्षिणपंथ के एक अग्रणी नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी की झाँकी लगी हुई थी। वहाँ 15 से 20 पैनल थे जिन पर उनके जन्म से लेकर शिक्षा-दीक्षा और सामाजिक-राजनीतिक जीवन का विवरण दर्शाया गया था। कुछ पैनलों पर 1930 और 1940 के दशक में हिन्दू महासभा के साथ उनकी सक्रियता दिखाई गई थी और कुछ पैनल उनके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर केन्द्रित थे। एक भी पैनल ऐसा नहीं था जिसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए किसी भी आन्दोलन या स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भागीदारी अथवा उससे उनके किसी भी सम्बन्ध का ज़िक्र हो।
औपनिवेशिक चरण का कहीं ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट उदाहरण हमें 1920 के दशक के मध्य में स्थापित गीता प्रेस में मिलता है, जिसका घोषित लक्ष्य सनातम हिन्दू धर्म की रक्षा और उसका प्रचार करना था लेकिन उसका प्रच्छन्न राजनीतिक एजेंडा उसकी पत्रिका ‘कल्याण’ में छपता था। स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक भारतीय राष्ट्र बनाने को लेकर जो सहमति थी उस पर गीता प्रेस बहुत आक्रामक तरीक़े से सवाल करता था जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू महासभा की सहमति और भागीदारी शामिल थी।
[…]
आजकल हम यह भी सुनते हैं कि देश बदल चुका है और इस ‘नये’ भारत के साथ हमारी यह विरासत शायद अप्रासंगिक हो चुकी है। यहाँ तक कि आजकल गांधी को भी पुराना मान लिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि अब गांधी से दशकों पुराने मोह को हमें छोड़ देना चाहिए। जाहिर है कि आज़ादी के बाद बीते दशकों में यह देश लगातार बदलता रहा है, इसके बावजूद राष्ट्र-निर्माण के कुछ बुनियादी उसूल ऐसे हैं जो हमेशा प्रासंगिक और वैध रहेंगे। हमारे राष्ट्रवाद ने सभी भारतीयों के सामूहिक गौरव का प्रतिबिम्बित किया है। कोई ऐसा नागरिक नहीं रहा जो धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के चलते इसके दायरे से बाहर छूट गया महसूस करता हो। जैसा कि गोपालकृष्ण गांधी ने कहा था, “भारत सभी भारतीयों से है और सभी भारतीय मिलकर भारत हैं।” यही भावना हमारे संविधान के मूल में है। इस मूलभूत भावना से कोई भी विचलन इस राष्ट्र के निर्माता लोगों के बीच असहजता और असुरक्षा को पैदा करेगा। यह आइडिया ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रवाद गहन विमर्श और मन्थन का परिणाम था जिसकी शुरुआत बीसवीं सदी के आरम्भ में हुई। आज इसी उदार राष्ट्रवाद का सत्त्व दाँव पर लगा हुआ है, जिसे इस राष्ट्र ने पिछली सदी के दौरान पाला-पोसा था।
तेज़ी से बदलते हुए इस ताने-बाने में ज़रूरत है कि हम गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रवाद और संस्कृति की अवधारणाओं पर आत्ममन्थन करें। हमें वापस उन मूल विवरणों और परिभाषाओं की तरफ़ जाने की ज़रूरत है जो हमारे नेताओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में दी थीं। हमें मूल अभिलेखों को देखना होगा और राष्ट्र, राष्ट्रवाद और संस्कृति को परिभाषित व सूत्रबद्ध करने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना होगा। इन अभिलेखों में हम पाएँगे कि कई जगह राष्ट्रवाद और देशभक्ति को एक दूसरे के पर्याय की तरह प्रयोग किया गया है, दोनों के बीच फ़र्क़ धुँधला गया है। यहाँ मैं दोनों के बीच अन्तर को स्पष्ट करना चाहूँगा। देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के प्रति लगाव और उसकी रक्षा करने की इच्छा, जबकि राष्ट्रवाद देश के प्रति एक कहीं ज़्यादा अतिवादी समर्पण का रूप है। इसीलिए राष्ट्रवाद की मुख्य कमी यह है कि यह लोगों को अन्धा कर सकता है। अपने देश के प्रति प्रेम तो ज़रूरी है ही, लेकिन यह प्रेम यदि संवैधानिक मूल्यों या जनतांत्रिक आदर्शों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो यह विकृत हो जाता है।