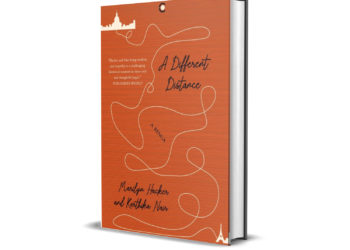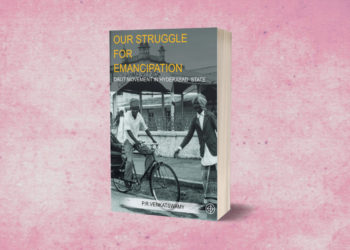मुकुल शर्मा की किताब दलित और प्रकृति : जाति और पर्यावरण आंदोलन (वाणी प्रकाशन, पेपरबैक संस्करण, 2022) इस अर्थ में विशिष्ट है कि यह पर्यावरण के अध्ययन में पहली बार जाति, सत्ता, ब्राह्मणवाद और दलित स्वर के जटिल अन्त:सम्बन्धों की गहन पड़ताल करती है। यह प्रकृति और पर्यावरण की चर्चा करते हुए दलितों के दृष्टिकोण, उनके स्वरों और उनके संगठनों ने किस तरह एक पर्यावरणीय संवदेना को निर्मित किया है उसकी पड़ताल करती है, जिसमें देश के कई हिस्सों में प्रचलित विविध सांस्कृतिक विधाओं, लोकाचारों, लोकप्रिय संस्कृतकर्मियों और उपलब्ध साहित्य के शोध का सहारा लिया गया है। यह पुस्तक सिर्फ एक प्रदेश या कुछ इलाकों से नहीं बल्कि देश के विविध हिस्सों से प्रकृति के साथ दलितों के अंत:सम्बन्धों को बहुत ही तफ़्सील से सामने लाती है। जैसा कि पुस्तक में कहा गया है, “यह मौक़ा-ए-अध्ययन के ज़रिये दर्शाती है कि किस प्रकार देश की पर्यावरण राजनीति जाति-वर्चस्व का वरण करती है। और स्वच्छता और शौच पर काम करने वाले कुछ पर्यावरणीय संगठन और सोच ‘पर्या-जातिवरण’ के तहत दलितों की मुक्ति और पुनरुत्थान के लिए नव-हिन्दुत्ववाद का जाला बुनते हैं, जिसमें ब्राह्मणवाद के स्वरूप और नेतृत्व की जय-जयकार होती है।” पुस्तक में पेरियार, फुले और अम्बेडकर के विचारों और कार्यों को पर्यावरण की दृष्टि से भी देखा गया है।
किताब का कुछ अंश प्रस्तुत है।

ओ अश्वेत लड़की
तुम काटती हो गेहूं की फसल
तुम्हारे हंसुए काटते हैं हर फसल
आओ! काली के रौद्र के साथ आओ!
ओ अश्वेत शेर के बच्चे
तुम मिट्टी को काला रंग देते हो
तुम हो शेर और तेंदुए के बच्चे
ईमारते के गारे के साथ
काला की रस्सियों के साथ
आओ लम्बे डग भरते हुए असुरों की तरह!
तुम बन गए हो मिट्टी के खाद
नदी के रंग
तुम्हें जीते जी धकेला गया है
कीचड़ के नीचे गारे की तरह
जैसे कई पूलया के सर काटे गए
और खेतों और मैदानों में उनके खून बहाए गए।
-के.के.एस.दास, मलयाली दलित लेखक
[…]
वेद मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मण आहुति देने लगे
अब बलिदान विधि का मुहुर्त आ गया
रक्त के फब्बारे छूटे, पोखर से भी पानी की धारा छूटी…
पानी नहीं वह थी कृपा प्रभु की
वह था अछूतों का उद्धार रे…
जिसके रक्त का बना पानी रे…
उसी पानी से नहाए शिवती…नहाए ब्राह्मण
राजा-प्रजाजन सब नहाए रे…
दुखों को जिसने दूर किया था
बारहवीं सदी का तू संत कहलाया,
महासप्तमी प्रकाशित
लेकिन समाज ने उसकी कद्र कभी न की
-मायावेल, एक गुजराती दलित लोक गीत जिसमें एक अभिशप्त, सूखे तालाब में पानी लाने के लिए दलित माया के बलिदान की गाथा गायी गई है।
[…]
जाति और प्रकृति भारत में आन्तरिक और जटिल रूप से जुड़े हैं, फिर भी इनके अन्तर्सम्बन्धों की कोई समीक्षा नहीं हुई है। सच यह है कि एक श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था में दलितों के रोजाना अनुभवों और वृत्तांतों में प्रकृति के बोझ भरे हैं। जमीन की छवियों में जाति द्वन्द जनित श्रम, रक्त और दासता सजीव होते हैं। सूखे इलाकों में दलितों को पोखरों और जल स्रोतों के पुनःभरण के लिए अनिवार्यतः अपनी बलि देनी है। विभिन्न स्थलों और स्थानों में – गांव से शहर, मंदिर से स्कूल – प्रदूषण, अशुद्धि और गंदगी जैसे जाति के रूपक दलितों की मौजूदगी-भर से भारी खतरे की आशंका बताते हैं। जंगल दलितों के लिए या तो स्वर्ग, नहीं तो नरक साबित होता है। नदी मुर्दे को विसर्जित करने की जगह है। भय और हिंसा, आंतक और हाड़-तोड़ मेहनत, खून-खराबा और युद्ध से करीबी से जुड़ी प्रकृति के साथ दलितों के अनुभव अलग और विशिष्ट हैं। उदाहरण के लिए केरल के भूमिहीन खेत मजदूरों के गीतों में जगंल, जानवर, लकड़ी और मौसम की ऐसी स्मृतियां हैं :
जंगल में लकड़ियां चुनते
जंगली जानवरों से सामना
मौसम है हमारे खिलाफ
साथ-ही-साथ दलितों के पर्यावरण अनुभवों की अपनी ज्वलंतता और गतिशीलता है। प्रकृति के साथ अपना जीवन जीते हुए वे लगातार जाति आधिपत्य से संवाद और संघर्ष करते हैं और पर्यावरण की कल्पना चित्र भी उकेरते हैं। दलित चिन्तकों और समकालीन दलित स्मृतियों की दुनिया में हमें पर्यावरण के इर्द-गिर्द विविध और सशक्त सामाजिक और स्थानिक रूपक मिलते हैं। यह किताब प्रकृति में दलितों के अपनी जगह की खोज की पड़ताल करती है। यह दलितों की अलग-अलग आवाजों – अतीत के बंधुआ मजदूरों के गान और बयान, अग्रणी दलित बुद्धिजीवियों, नेताओं और लेखकों की रचनाओं, दलितों के प्रकृति आधारित रूपक और स्मृतियां, उनके आन्दोलनों, संगठनों, आगाजों के जरिए दर्शाती है कि किस प्रकार जाति-सांचित प्रकृति में दलित अपने को पहचानने और बतलाने की विविध कोशिशें करते हैं। किताब में ‘दलित’ का प्रयोग एक व्यापक, बहुआयामी, संयुक्त पद के रूप में किया गया है जिसमें कभी मछुआरे, नाविक, नटी भी शामिल हैं। प्रकृति-जाति विरोधाभास का फलक व्यापक है जो वंचितों के स्व, शरीर, सान्निध्यता, अवस्था को प्रभावित करता है। जाति और प्रकृति का ऐसा गूथन भारतीय पर्यावरणवाद के लिए गंभीर चुनौती है जिसमें इन सम्बन्धों की अब तक अनदेखी की गई है। यह अध्ययन पर्यावरणवादियों की इस रिक्तता को भरने की कोशिश करता है। साथ-ही-साथ, प्रकृति और दलितों के जटिल रिश्तों के अध्ययन से पर्यावरण और दलित, दोनों के कुछ नए पहलू उजागर होते हैं। यह अध्ययन मुख्यतः तीन आधारों पर टिका है जिसके जरिए दलित और पर्यावरण की जातिगत संकल्पनाओं को समझने की कोशिश की गई है। पहला, भारत में बलवान और बेसंकोच ब्राह्मणवाद और पर्यावरणवाद की एक विशेष धारा। दूसरा, दलित पर्यावरण सोच – मिथक, उपाख्यान, सैद्धान्तिक और सचेतन। और, तीसरा, दलित आन्दोलन और संगठन जिसके नई सार्वजनिकता और सामूहिकता जैसी कुछ आत्मसात धारणाएं हैं। इन तीनों आधारों में आपसी सम्बन्ध है जिनके जरिए दलित पर्यावरणवाद का एक व्यापक फलक – पर्यावरणीय संघर्ष और समायोजन सिद्धान्त और प्रयोग – देखा गया है। हमें पता चलता है कि किस प्रकार पर्यावरण के दलित अर्थ नव-ब्राह्मणवाद के विचारों और व्यवहारों और पर्यावरणवाद की कुछ धाराओं को चुनौती देते हैं। हमारे सामने यह तथ्य भी उभरकर आता है कि तमाम अस्पष्टताओं और विविधताओं के बावजूद दलित विचारों में स्थानिक समानता के रूप में पर्यावरण की एक नई समझदारी और जाति के बोझ से मुक्त पर्यावरणवाद मौजूद है। अध्ययन में कोई एक इकहरा दलित विचार या पर्यावरण की एक मुकम्मल समझ नहीं है बल्कि इसमें ऐसे बहुल और समृद्ध बौद्धिक संसाधन हैं जिससे प्रकृति को एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक टेक मिलती है।