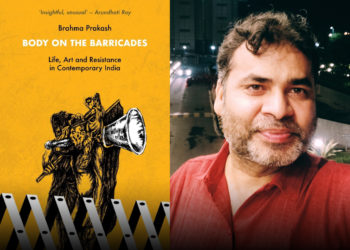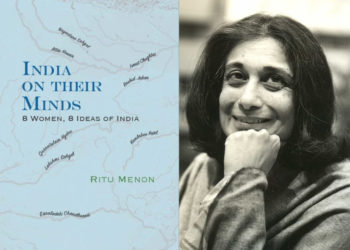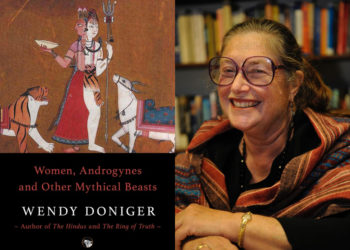रंगमंच निर्देशक और निर्माता सुनील शानबाग लेखिका गीता हरिहरन के साथ बातचीत में असहमति के विचार से रू-ब-रू होते हुए सेंसरशिप की उन कई परतों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने आज हमें जकड़ा हुआ है। वह असहमति को बदलाव की एक ऐसी मजबूत ताकत के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जिसे जिंदगी से पृथक करना मुश्किल है। वह रंगमंच में सामूहिकता के साथ काम करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में भी बात करते हैं। रंगमंच में भाषा किस तरह से एक प्रमुख भूमिका निभाती है और इस विशाल बहुभाषी देश में एक नाटक किस तरह से अपनी यात्रा करता है, वह इस पर भी रोशनी डालते हैं। सुनील शानबाग और गीता हरिहरन की इस बातचीत का यह दूसरा और अंतिम भाग है।

गीता हरिहरन (जी.एच.) : आपके विचार में असहमति क्या है? रंगमंच से जुड़े व्यक्ति/फिल्मकार और एक नागरिक के रूप में यह आपके जीवन को कैसे जोड़ती है?
सुनील शानबाग (एस.एस.) : मेरे हिसाब से असहमति रचनात्मक और बदलाव की एक ऐसी मजबूत ताकत है जिसे स्वयं के जीवन से अलग करना मुश्किल है। कला की आवश्यकता है कि आप प्रश्न करें, सामान्य से लेकर अति गंभीर तक। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं इसे किसी दूसरे तरीके से कह सकता हूं।
जी.एच. : एक खास तरह के नाटक के मंचन के माध्यम से व्यक्त अहसमति, जिसमें (मंचन) नाटककार (या पाठ) से लेकर निर्देशक और कलाकारों तक की सामूहिकता शामिल होती, किस तरह से इसे प्रभावित करती है?
एस.एस. : बिल्कुल, रंगमंच एक सामूहिक कार्य है, और इस तरह के सभी कार्य बातचीत की श्रृंखलाओं पर निर्भर करते हैं। एक आदर्श स्थिति में, इसमें शामिल सभी लोग चीजों को एक ही दिशा की ले जा रहे हैं और यह अभिव्यक्त किए जा रहे विचारों में समृद्धि और विविधता में अपनी भागीदारी निभाता है। कई बार स्थिति इतनी सहज नहीं होती है। लेकिन बातचीत से अक्सर दिलचस्प चीजें सामने आती हैं, जिनकी प्रक्रिया की शुरुआत में कल्पना तक की नहीं गई होती है। हम जब लिखने से पहले पाठ पर कार्य करते हैं, तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले विचारों को सामने रखा जाता है। इसलिए एकदम शुरुआत में हर किसी को पाठ में शामिल किया जाता है। लेकिन एक प्रक्रिया जो किसी रूप को आकार देने में शामिल है, लेकिन कमरे में जो लोग होते हैं उसमें हर कोई उस तरह खुले तौर कहने के लिए सक्षम नहीं होता या इच्छुक नहीं होता, जिस तरह से कोई अन्य व्यक्ति होता है। इस पर कोई किस तरह से प्रतिक्रिया जताता है? क्या हम इच्छुक नहीं होने या अक्षमता को एक बाधा के रूप में देखते हैं? क्या हम रचनात्मक और सम्मानजनक समाधान तलाशने के लिए इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं? मैं हमारे कार्य और अन्य के कार्य, दोनों ही तरह की स्थिति से वाकिफ हूं और अलग-अलग लोग भिन्न-भिन्न तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मेरा मानना है कि जब तक अच्छी भावना होती है, तो रचनात्मक समाधानों को तलाशा जा सकता है। इसके अलावा, एक कलाकार के रूप में हमें स्वयं को लगातार यह याद दिलाने की जरूरत है कि एक विशिष्ट कार्य जो हम करेंगे वह अंतिम कार्य नहीं है! फिर एक और काम करने का अवसर आएगा, और फिर उसके बाद एक और आएगा। इसलिए हमें शांत रहना सीखना चाहिए…यह दुनिया का अंत नहीं है।
जी.एच. : क्या हमारी बहुभाषी स्थिति देश के भीतर “स्थानीय” रंगमंच की यात्रा में अड़चन पैदा करती है? या हमारे पास अनुकूलन के दृष्टांत हैं जो वास्तव में स्थानीय (रंगमंच) को समृद्ध करते हैं?
एस.एस. : साठ के दशक में और सत्तर के दशक की शुरुआत में अखिल भारतीय रंगमंच के कार्य को लेकर अधिकतर जागरूकता विभिन्न भाषाओं में लिखे गए नाटकों के अनुवाद के आधार पर निर्मित की गई थी। अनुवाद ने प्रोडक्शन और विभिन्न क्षेत्रीय संवेदनाओं एवं विचारों को प्रोडक्शन में समाहित करके उसे दर्शकों तक पहुंचाया। जिन्होंने समकालीन भारतीय रंगमंच समुदाय के एक हिस्से के रूप में खुद को देखा, उनके जुनून और पहलकदमी की वजह से यह हो पाया। नाटककारों ने एक-दूसरे के नाटकों का अनुवाद किया, और इन अनुवादों को प्रसारित किया गया और उनका पाठ किया गया। मेरा मानना है कि स्वामित्व, जिम्मेदारी और उदारता की इस तरह की भावना महत्वपूर्ण है। उस वक्त के प्रमुख नाटककारों के कार्यों को अनुवाद की वजह से पूरे देशभर में जाना गया। जब मैं 1974 में रंगमंच से जुड़ा, तो एक कलाकार के रूप में मेरा पहला नाटक एक मराठी नाटक के हिंदी अनुवाद पर आधारित था, और उसके बाद अगले कुछ वर्षों तक मैंने कन्नड़ और बांग्ला के नाटकों के अनुवादों पर आधारित नाटकों में काम किया।

लेकिन अब आपके सवाल पर वापस लौटते हुए, मैं यह कहूंगा कि एक विशाल बहुभाषी देश में एक नाटक किस तरह से अपनी यात्रा करता है, और उसमें भाषा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। लेकिन यह कभी-कभी ऐसे विकल्प को चुनने की ओर ले जाता है जो नाटक की सांस्कृतिक विशिष्टता के साथ समकालिक नहीं होता है। उदाहरण के लिए, “कॉटन 56, पॉलीएस्टर 84” के लिए नैसर्गिक भाषा मराठी थी, क्योंकि मेरी रंगमंच की यात्रा एक जगह से दूसरी जगहों पर काफी ज्यादा होती है, इसलिए नाटक को ऐसी भाषा में करना युक्तिपूर्ण था जिसे व्यापक तौर पर समझा जाता। लेकिन तब चुनौती यह थी कि हिंदी में नाटक करते हुए मराठी के मूलतत्व को किस तरह से बनाए रखा जाए।
यहां तक कि मुंबई जैसे महानगर में भी बहुत सारी भाषाएं एक साथ बसर करती हैं, हमारे रंगमंच के दर्शक और हमारे प्रदर्शन स्थान बहुत एकांगी या अलग-थलग से होते हैं। उदाहरण के लिए, मराठी नाटकों के लिए एक अलग दर्शक वर्ग है और गुजराती के लिए अलग। और इसी प्रकार अन्य भाषाओं के नाटकों के लिए भी प्रदर्शन स्थल समर्पित हैं। लेकिन साथ ही साथ नाटकों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद भी होता है और उनका मंचन भी होता है। और आखिरकार कुछ नाटक जरूर ऐसे होते हैं जो ज्यादा व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यह परम आवश्यक है कि अनुवाद किसी न किसी रूप में प्रकाशित किए जाएं, दूसरों के साथ साझा किए जाएं और उन्हें व्यापक रूप से तथा आसानी से उपलब्ध कराया जाए। और यही एक मुश्किल तथा महत्वपूर्ण कार्य है।
जी.एच. : आपने अपने काम में सेंसरशिप के साथ जीने और अनुभव करने का एक विशेष विषय निर्मित किया है। क्या आप हमें सेंसरशिप की उन परतों से अवगत करना चाहेंगे जो आज हम पर लागू होती हैं, और इसके अलावा प्रतिरोध करने की कुछ रणनीतियों से भी?
एस.एस. : जब हम “सेक्स, मॉरेलिटी और सेंसरशिप” के संबंध में सेंसरशिप के विचार पर शोध कर रहे थे, तब नाटककार जी.पी. देशपांडे के साथ हमारी एक बहुत लंबी बातचीत हुई और उन्होंने बहुत ही विद्वतापूर्ण तरीके से तथा गहरी विचारशीलता के साथ हमारे सामने इस विषय को खोला। उन्होंने जो बहुत सारी बातें कही, उनमें से एक विशेष बात जो रंगमंच से जुड़े होने के कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, वह यह थी कि राज्य के औपचारिक संस्थानों द्वारा लगाई गई सेंसरशिप और भीड़ तथा समाज के द्वारा लगाई गई अनौपचारिक सेंसरशिप के बीच का फर्क। औपचारिक सेंसरशिप में तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक सेंसरशिप में ऐसी कोई संभावना नहीं होती। समाज द्वारा लगाई गई (नैतिक) सेंसरशिप बहुत ही घातक और चतुराई से भरी हुई होती है, और हम इसका उन्मूलन केवल शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की एक लंबी और अविरल प्रक्रिया के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन भीड़ की सेंसरशिप से कैसे निपटा जाए? वहां तर्कपूर्ण बातचीत के लिए कोई स्थान नहीं होता। अक्सर हिंसा की धमकियां होती हैं और कानून बड़ी ही आसानी से स्वयं को ‘कानून और व्यवस्था की स्थिति’ को बनाए रखने के नाम पर झुका देता है। जिसके चलते वह कलाकारों की एवज में हमलावरों को शक्तिशाली बना देता है। सेंसरशिप का यह रूप आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसे न्याय और कानून की प्रक्रिया को तोड़ने-मरोड़ने के नजरिये से बहुत सक्रिय प्रोत्साहन एवं समर्थन मिलता है। हमले के इस स्वरूप में एक धुंधलापन या एक अस्पष्टता निहित होती है। अक्सर देखा गया है कि इस खेल में और भी एजेंडे होते हैं। कला के एक स्वरूप पर हमला इस बात पर नहीं है कि उसने किसी की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाई है, बल्कि यह जबरन वसूली का एक सीधा-साधा मामला है। जैसे ही पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचता है, हमले वापस ले लिए जाते हैं। इस प्रकार का पागलपन समाज के ताने-बाने को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और इसकी निंदा जितने भी कड़े शब्दों में की जाए, वह कम है। इसके अलावा, वास्तविकता यह है कि बहुत सारे कलाकार सेंसरशिप के विचार का समर्थन करते हैं। हम महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। रंगमंच पर नजर रखने वाला बोर्ड को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे वह सार्वजनिक नैतिकता का एक प्रबुद्ध और हितैषी रक्षक हो!

ऐतिहासिक रूप से, रंगमंच से जुड़े लोगों ने सेंसरशिप से बचने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों को यह काम औपचारिक संस्थानों के साथ बातचीत और वचनबद्धता से करना पड़ता है। कुछ के पास कलात्मक रणनीतियां होती हैं। और कुछ लोगों को ऐसा करने के लिए यह देखना पड़ता है कि वह अपने काम को किस दर्जे पर माप रहे हैं – जो उन्हें अनुमति देता है कि वे रडार से बचे रहें।
अपने खुद के कामकाज में, जब कलात्मक स्वतंत्रता के विषय पर किसी सार्वजनिक विमर्श में शामिल होना संभव था, तो मैंने तुलनात्मक रूप से ज्यादा उदार दौर देखा है, और अब मैं एक बहुत ही सनक से भरा हुआ तथा असहिष्णु दौर देख रहा हूं जिसमें ऐसा कोई भी विचार पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और कला से जुड़ा समुदाय घेरेबंदी की स्थिति में आ गया है। हमें यह विश्वास रखना होगा कि चीजें बदलेंगी, लेकिन यह तभी होगा जब हम आज के इस क्षण में बच पाएंगे और बिना अपनी ईमानदारी को खोए काम करते रहने के तरीके ढूंढ पाएंगे।
जी.एच. : कोविड महामारी ने हमें दिखाया है कि सांस्कृतिक कर्मियों के बीच में समुदाय और एकजुटता की भावना को निर्मित करना कितना महत्वपूर्ण है। हम उन प्रयासों, जिसमें आप जैसे लोग शामिल रहे हैं, को कैसे कायम रखेते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके जरिये हम राज्य की संस्थाओं पर ज्यादा मददगार होने के लिए दबाब डाल सकते हैं?
एस.एस. : इस महामारी ने हमारे सबसे खराब भय और विश्वास को सच साबित कर दिया कि राज्य के संस्थानों की कला अथवा कलाकारों में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। इस महामारी के दौरान कलाकारों द्वारा झेली गई खौपनाक मुश्किलों की तरफ उनकी ये असंवेदनशीलता हमारी कल्पना के भी परे थी। जहां थोड़ा-बहुत समर्थन दिया भी गया था तो वहां कलाकारों को अत्यधिक अपमान और असम्मान का भागीदार बनाया गया। हमारे जाने-माने प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों ने कलाकारों को राज्य द्वारा प्रायोजित सर्जिकल स्ट्राइक दिवस जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दबाब डाला! और यह महामारी के दौरान हुआ।
जब तक कलाकारों को उचित स्थान नहीं दिया जाता, विशेषकर उन कलाकारों को जो औपचारिक संस्थानों में भागीदारी करने की अपनी प्रक्रिया के परे ज्यादा व्यापक मुद्दों को देखने-समझने की क्षमता रखते हैं, मैं समझता हूं कि राज्य के साथ काम करने की कोशिश केवल समय की बर्बादी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे संस्थान अपने सार्वजनिक चरित्र के अनुरूप अपना फर्ज निभाने के लिए बाध्य हैं। लेकिन उनके साथ काम करने का हमारा अपना अनुभव बहुत ही बुरा रहा है। और सच में, समुदाय बनाने और एक-दूसरे को समर्थन के तरीके ढूंढने में हमारे समय का बेहतर उपयोग होता है। हमको व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हम हमारे द्वारा निर्मित इस सांस्कृतिक पूंजी का राज्य द्वारा उपयोग करने का विरोध कर सकें।
कृष्ण सिंह द्वारा हिंदी में अनुवादित। अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ें।