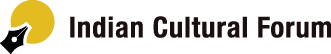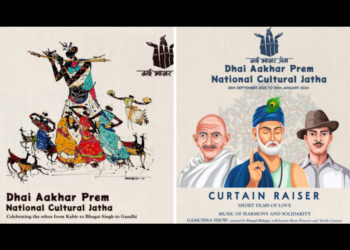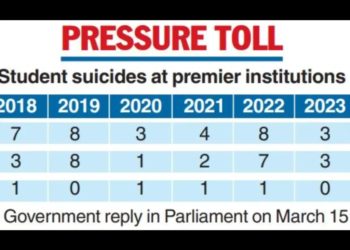सैकड़ों पत्रकार और सहयोगी-प्रेस-कार्मी सड़कों पर हैं, ख़बरों से जुड़े दफ़्तरों में से तक़रीबन आधे दफ़्तर बंद हैं। कई पत्रकार घर से काम कर रहे हैं, और भारत में मीडिया पर बढ़ते हमलों के इस माहौल के बीच वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम रिपोर्ट 2022 आती है, जो कि सही मायनों में आज के भारतीय प्रेस की आज़ादी को लेकर एक झटका है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2021 में 142 से गिरकर इस साल 180 देशों में से 150 हो गयी है। 2016 में भारत 133वें स्थान पर था।
इस सूचकांक से नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में मीडिया की स्वतंत्रता में लगातार आयी गिरावट दर्ज हो रही है। यह सूचकांक रिपोर्टरों और समाचार संस्थाओं की “बिगड़ती स्थिति” की बात करता है। इस सूचकांक में कहा गया है कि लोकतांत्रिक रूप में जाने जाते देशों के बीच भारत का मीडिया कहीं ज़्यादा “तेज़ी से हो रही सत्तावादी और / या राष्ट्रवादी सरकारों” के दबाव का सामना कर रहा है।
हक़ीक़त में वास्तविकता कहीं ज़्यादा विकट है। इस तथ्य पर विचार करें कि हम एक ऐसे ‘अघोषित आपातकाल’ में हैं, जो 2016 से लगातार बढ़ ही रहा है। प्रेस की आज़ादी को झटके देने वाले 1975 का भयानक घोषित आपातकाल महज़ 21 महीने तक ही चला था। सरकार का मीडिया को डराना-धमकाना आज एक ख़ास विशिष्टता बन गया है। पत्रकारों और संपादकों के ख़िलाफ़ ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में झूठे मामले दर्ज किये जा रहे हैं। कुछ पत्रकार ऐसी रिपोर्ट लिखने के लिए देशद्रोह के मामलों का सामना कर रहे हैं, जो कि सत्ता के हिसाब से नहीं होती हैं।
पत्रकारों के ख़िलाफ़ ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) जैसे सख़्त क़ानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि श्रीनगर में फ़हद शाह और उत्तर प्रदेश में सिद्दीक़ी कप्पन के मामले में हुआ था, दोनों इस समय भी निवारक नजरबंदी के तहत जेल में हैं।
मीडिया पर बढ़ते हमलों और डराने-धमकाने के कुछ अन्य स्पष्ट संकेत निम्नलिखित हैं:
1. सांप्रदायिक चरमपंथी गिरोहों की ओर से मीडिया कर्मियों पर ख़ासकर भाजपा शासित राज्यों में शारीरिक हमले हुए हैं।
2. मीडिया को धमकाने की सरकार की कोशिशों ने आर्थिक अपराधों के साथ-साथ हुक़्म नहीं मानने वाले मीडिया घरानों को निशाना बनाने का रूप ले लिया है। आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों का अक्सर ऐसे मीडिया घरानों के प्रबंधन को परेशान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
3. सरकारी नियंत्रण और सेंसरशिप बढ़ाने की कोशिश सभी तरह के मीडिया तक फैली हुई हैं। डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों के प्रसार को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नये नियम 2021 में पेश किये गये थे, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर विषय-सामग्री को निर्देशित करने और सरकार को लगने वाली आपत्तिजनक डिजिटल समाचार सामग्री को हटाने के अधिकार दिये जाने की इजाज़त देते हैं। समाचार चैनलों पर सीमित समय के लिए या स्थायी आधार पर प्रतिबंध लगाकर मीडिया का मुंह बंद करने की भी कोशिश की जा रही है।
कॉरपोरेट और बड़े व्यापारिक घरानों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले मीडिया के स्वामित्व की प्रकृति में बदलाव लाकर मीडिया की आज़ादी और निष्पक्षता से जिस तरह समझौता किया जा रहा है, वह एक अशुभ संकेत हैं। यह बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं ज़्यादा साफ़ तौर पर देखी जा सकती है, जहां कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये,तो मोदी सरकार की ओर से मीडिया को मौजूदा हुक़ूमत के पक्ष में ढोल पीटने वाले के रूप में अपना सहयोगी बनाया जा रहा है। इससे भी बदतर तो यह है कि इनमें से कुछ मीडिया घरानों ने हिंदुत्व के सांप्रदायिक प्रचार को आक्रामक रूप से घर-घर पहुंचाना शुरू कर दिया है, जो कि साफ़ तौर पर कॉर्पोरेट-हिंदुत्व वाले एक गठजोड़ की तरफ़ इशारा करता है।यह प्रवृत्ति हिंदी मीडिया के साथ-साथ उर्दू प्रेस के कुछ हिस्सों में भी ज़्यादा दिखायी देता है। कुल मिलाकर, लोकतंत्र का मज़ाक बनाया जा रहा है। चाटुकारिता और ज़बरदस्त साम्प्रदायिक दुष्प्रचार आज एक आम प्रचलन बन गया है।
इसके अलावा, जो पत्रकार और मीडिया संस्थायें निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं और संपादकीय स्वतंत्रता बनाये रखना चाहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि उन्हें “हुक़ूमत की अजीब-ओ-ग़रीब ताक़त वाली भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।” 1975 का आपातकाल और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की मीडिया पर की गयी वह टिप्पणी याद है? उन्होंने कहा था, “उन्हें झुकने के लिए कहा गया था और वे रेंगने लगे थे।” हालात अब कहीं ज़्यादा बिगड़ रहे हैं।
प्रेस फ़्रीडम रिपोर्ट बताती है कि हर साल औसतन तीन या चार पत्रकार अपने काम के सिलसिले में मारे जा रहे हैं (जनवरी 2022 से लेकर अबतक एक पत्रकार मारा गया है और 13 पत्रकार इस समय जेल में हैं)। इस रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत दुनिया के “मीडियाकर्मियों के लिए सबसे ख़तरनाक देशों” में से एक है।
हालांकि, यह असली कहानी का महज़ एक हिस्सा भर है। पत्रकारों, कलाकारों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं आदि पर नज़र रखने के लिए इज़रायली स्पाइवेयर पेगासस के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाये जा रहे हैं और जवाबों को टाला जा रहा है।
अन्य ख़तरों के संकेत भी हैं और वह यह कि भारत की राजधानी में केंद्रीय प्रेस मान्यता की मंज़ूरी की प्रक्रिया को दूसरे प्रतिबंधों के साथ-साथ मुश्किल बना दिया गया है, जिससे संसदीय मामलों की कवरेज में कमी आ गयी है। यहां तक कि कभी प्रतिष्ठित पत्रकारों की रही लंबी और प्रतिष्ठित श्रेणी को भी बदल कर एक चुनिंदा तमाशा बना दिया गया है। केंद्र और दिल्ली प्रांत, दोनों ही सरकारों की मान्यता समितियों से जिन ज़्यादातर निकायों को मान्यता मिलती है,उनमें सरकारी चयनात्मकता के लक्षण साफ़-साफ़ दिखायी देते हैं।
उर्दू प्रेस
उर्दू प्रेस के 200 साल हो गये हैं और इसने असल में आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभायी है, लेकिन आज विज्ञापन के दबाव और कुछ अन्य बदलावों के चलते वे अपने वजूद के लिए हांफ रहे हैं। कई तो बिक चुके हैं।
एक वक़्त था, जब लोग यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (UNI) की छत्रछाया में एक जीवंत उर्दू समाचार सेवा की बात करते थे। आज यहां तक कि वेतन कटौती, लंबित वेतन और पूर्व पत्रकार जो छोड़ चुके हैं या जाने के लिए मजबूर हैं, उन्हें मुआवज़े के लिए इंतज़ार कराते हुए यूएनआई को भी व्यवस्थित रूप से ख़त्म किया जा रहा है। अब समय-समय पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (PTI) भी भारी सरकारी दबाव में है, जबकि कुछ निजी समाचार और टीवी एजेंसियां सरकारी संरक्षण में पल-बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुस्तान समाचार को भी नया रूप-रंग दे दिया गया है और एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल एएनआई के लिए सरकारी संरक्षण की बात तो आम तौर पर की ही जाती है।
ये सब ख़बरों के सांप्रदायिकरण के गंभीर ख़तरों की ओर इशारे करने वाले अशुभ संकेत हैं। जैसा कि द वायर में बताया गया है कि 21 महीनों तक चली इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय आपातकाल में सेंसरशिप, भारतीय प्रेस परिषद का ख़ात्मा और पत्रकारों की गिरफ़्तारी होते देखा गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पत्रकारिता को उस पैमाने पर अपराधीकरण किया है, जो कि 1977 के बाद से नहीं देखा गया है, प्रशासनिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रेस परिषद को अप्रासंगिक बना दिया गया है और आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन की रोकथाम अधिनियम, 1976 की भावना को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। उस आईटी नियम, 2021 की घोषणा के ज़रिये मोदी का ‘अघोषित आपातकाल’ पहले से ही अपने आठवें साल भी चल रहा है, जिसके ज़रिये सरकार ने आपत्तिजनक माने जाने वाली डिजिटल समाचार सामग्री को हटाने के अधिकार को हड़प लिया है।
एक और ख़तरनाक़ प्रवृत्ति पत्रकारों और सहकर्मियों को अपनी पसंद की यूनियनों के साथ जुड़ने की आज़ादी को लेकर है। संसद में जल्दबाज़ी में पारित की गयी नयी श्रम संहिता समाचार उद्योग के लिए किसी भी वेतन निर्धारण प्रणाली के ख़ात्मे की शुरुआत का संकेत बन गया है और सही मायने में कई प्रबंधन ने तो इसे एक प्रत्याशा के तौर पर देखा है,क्योंकि पिछले मजीठिया पंचाट(Majithia Award) कुछ मामलों में तो तक़रीबन 10 सालों से अदालत में पड़े लंबित मामलों के साथ एक मज़ाक बना हुआ है। कोविड ने बड़े पैमाने पर छंटनी आदि के लिए एक और बहाना दे दिया है। असल में यह श्रम संहिता न सिर्फ़ देश में बड़े पैमाने पर श्रम को प्रभावित करती है, बल्कि सालों के संघर्ष के बाद हासिल कामकाजी पत्रकार अधिनियम, वेतन बोर्ड और सेवा नियम पर भी व्यापक रूप से असर डालती है। इससे नये ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण भी अब मुश्किल हो जायेगा।
सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) के उपाध्यक्ष जे.एस.मजूमदार के मुताबिक़, “भाजपा सरकार के तीन प्रमुख नव-उदारवादी उद्देश्य थे: पहला-तीन कृषि कानूनों की शुरूआत के ज़रिये कृषि का निगमीकरण; दूसरा- चार श्रम संहिताओं की शुरूआत के ज़रिये मौजूदा श्रम क़ानूनों का विध्वंस; और तीसरा-सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित सरकारी संपत्तियों का निजीकरण।
हाल ही में सीटू नेता ने मई दिवस के एक कार्यक्रम में कहा कि सितंबर 2020 में एक हफ़्ते के भीतर किस तरह संसद ने तीन कृषि क़ानून और चार श्रम संहितायें पारित क दी थीं। हालांकि,मोदी सरकार अपने पहले मक़सद में कृषि यूनियनों के एक मंच से हार गयी थी और उन क़ानूनों के ख़िलाफ़ लंबे और मज़बूत अभियान के चलते कृषि क़ानूनों को वापस लेना पड़ा था। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों का समर्थन हासिल था।
सरकार श्रम क़ानूनों को निरस्त करने और श्रम संहिताओं को अधिनियमित करने में कामयाब तो रही, लेकिन मज़दूर वर्ग के प्रतिरोध के सामने उन्हें अभी तक लागू नहीं कर पायी है।
मजूमदार ने कहा कि पत्रकारों को कई अधिकारों से वंचित कर दिया जायेगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा संहिता के ज़रिये कामकाजी पत्रकार अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है। ये वही अग्रणी श्रम क़ानून थे, जिन्हें नेहरू युग के दौरान अधिनियमित किया गया था। क्योंकि ये संहितायें कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच भेद करती हैं,इसलिए अब पत्रकारों को इन श्रम क़ानूनों के तहत उन अधिकारों से वंचित कर दिया जायेगा, जो आज भी वजूद में हैं। उन्होंने कहा कि इससे लड़ने की ज़रूरत है।
इसलिए, आम मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा एकता और पत्रकारों के व्यापक संभव राष्ट्रीय गठबंधन की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ हमें एक कहीं ज़्यादा स्वायत्त मीडिया आयोग की ज़रूरत है, जिसमें न्यायपालिका, जनता और संसद के बीच से विशेषज्ञ शामिल हों, प्रेस परिषद की जगह हमें एक ऐसी मीडिया परिषद की आवश्यकता है, जिसमें सरकार के आधिपत्य वाले निकाय नहीं,बल्कि टीवी नेटवर्क और अन्य नये मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सहित पूरे मीडिया को शामिल किया जाये।
अतीत पर एक नज़र
साल 1956 में लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम पारित किया था।उस अधिनियम के तहत मीडिया या किसी भी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के मुद्रण, प्रसारण या प्रकाशन के लिए अभियोजन से संरक्षित किया गया था। इस अधिनियम के पीछे स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस पार्टी के नेता फिरोज़ गांधी का दिमाग़ था। फ़िरोज़ गांधी ने 23 मार्च, 1956 को उस बिल का परिचय देते हुए कहा था, “हमारी संसदीय सरकार और लोकतंत्र की कामयाबी के लिए यह ज़रूरी इसलिए है ताकि लोगों की इच्छा ही प्रबल रहे, यह ज़रूरी है कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि इस सदन में क्या होता है। यह आपका सदन या मेरा सदन नहीं है, यह तो लोगों का सदन है। उनकी ओर से ही हम इस सदन में बोलते हैं या कार्य करते हैं। इन लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहते हैं और क्या करते हैं। इस रास्ते में जो कुछ भी आड़े आता है, उसे हटा दिया जाना चाहिए।”
फ़िरोज़ गांधी इस बात से निराश थे कि प्रेस ने बीमा घोटाले में शामिल उन लोगों के नामों का ज़िक़्र नहीं किया था, जिन पर राज्यसभा में चर्चा हुई थी। उन्होंने प्रेस को नाम छापने की चुनौती दे डाली थी, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था कि प्रेस को उस क़ानूनी बाधा से सुरक्षा मिले. जो उन्हें ऐसा करने की राह में बाधा बनती है। लेकिन, वह दौर ही अलग था। आज तो सेंट्रल हॉल भी प्रेस के लिए ‘नो गो’ एरिया बन गया है और संसद की कवरेज भी कम कर दी गयी है।
तीन से चार साल पहले भारत की राजधानी में एक संगोष्ठी और चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें कश्मीर के पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की जानी थी, साथ ही साथ उनका स्वागत भी किया जाना था,लेकिन कुछ दबाव में अनिश्चित काल के लिए उसे स्थगित कर दिया गया था।
अगर थोड़े में कहा जाये,तो इस समय दोतरफ़ा लड़ाई की ज़रूरत है।एक तरफ़ प्रेस की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है,तो दूसरी तरफ़, यूनियन की स्वतंत्रता को बचाने और उचित समयबद्ध स्थायी वेतन निर्धारण मशीनरी के लिए लड़ाई जारी रखने के सिलसिले मे यूनियन बनाने, एक मीडिया परिषद के साथ नैतिक मुद्दों को देखने और विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के मीडिया आयोग को व्यापक परिदृश्य की स्थितियों पर नज़र रखने वाले मीडिया की आज कहीं ज़्यादा ज़रूरत है।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें