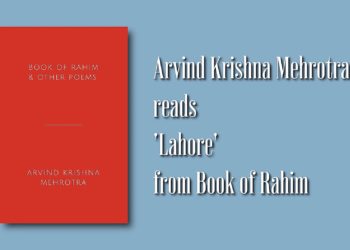कहा जाता है कि किसी इंसान की अहमियत तब समझ में आती है जब वह हमारी पहुंच से बाहर चला जाता है। मुक्तिबोध ने अपने जीवन काल में खुद की एक भी किताब प्रकाशित होते नहीं देखा, मगर आज वे हिंदी के सबसे प्रतीक्षित कवियों में से एक हैं।
देखा जाए तो ज़ुल्म के मूक दर्शक होने से ले कर उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने तक का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। हम तब तक चुप रहते हैं जब तक हम पर या हमारे चाहने वालों पर हमला नही होता। हम तब तक महफूज़ महसूस करते हैं जब तक खतरा हमारे दरवाज़ों पर नही खटखटाता।
आज वो खतरा हम सब के घरों की दहलीज़ पे पहुँच चूका है। चुप रहने से आवाज़ उठाने तक के इस सफ़र में एक धक्का और है बोल के इस हफ़्ते की पेशकश, मुक्तिबोध की कविता, “बहुत शर्म आती है”, मांडवी मिश्रा की बुलंद आवाज़ में।
बहुत शर्म आती है मैंने
खून बहाया नहीं तुम्हारे साथ
बहुत तड़पकर उठे वज्र से
गलियों के जब खेत खलिहानों के हाथ
बहुत खून था छोटी छोटी पंखुरियों में
जो शहीद हो गई किसी अनजाने कोने
कोई भी न बचे
केवल पत्थर रह गए तुम्हारे लिए अकेले रोने।