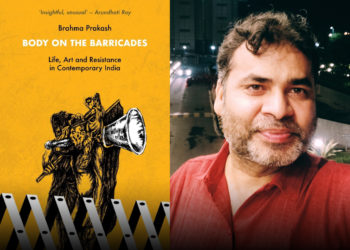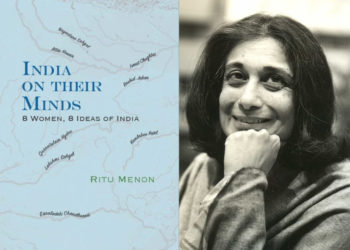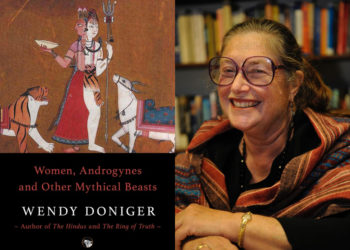सदियों से एक दूसरे में संचरित होने वाली बीमारियां मानव जाति के साथ हमेशा से मौजूद रही हैं। हालांकि, संक्रामक रोगों और महामारियों का मनुष्य को कृषि जीवन की तरफ़ जाने का एक ऐसा हालिया इतिहास रहा है,जिसने उन्हें एक-दूसरे के साथ क़रीब रहने के लिए प्रेरित किया है। जैसे-जैसे मानव सभ्यताएं आगे बढ़ती गयीं हैं, वैसे-वैसे ब्लैक डेथ, मलेरिया, तपेदिक, छोटा चेचक, पीलिया बुखार, हैजा जैसी पुराने प्रकार की बीमारियों से लेकर निपाह, ज़ीका, सार्स, कोविड-19 और इसी तरह के कई दूसरी तरह की बीमारियों के अनगिनत प्रकोपों से मानव जाति परेशान होती रही है।
महामारियों ने इतिहास के ढर्रे को अनेक तरीक़ों से बदला है, क्योंकि उन्होंने कुछ सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम को भी जन्म दिया है। वे हर समाज में विशिष्ट संकट और मसले पैदा करते रहे हैं। चिकित्सा इतिहासकार फ्रैंक स्नोडेन कहते हैं,”उनका [महामारी] अध्ययन करने के लिए समाज की संरचना, इसके जीवन स्तर और इसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को समझना ज़रूरी है।” उनका व्यक्तिगत रिश्तों, कला, साहित्य और दुनिया भर में विभिन्न तरह की मज़बूत हो चुकी ग़ैर-बराबरी और भेदभाव पर महत्वपूर्ण असर पड़ा है।
इन सभी बातों को समझने के लिए इंडिया कल्चरल फ़ोरमभारतीय इतिहासकारों के साथ एक लघु श्रृंखला शुरू कर रहा है। पहले फ़ीचर में मुकुलिका आर ने रोमिला थापर से इस महामारी के दौरान और कोविड -19 के बाद की दुनिया में लोकतंत्र की कल्पना को लेकर बात की है।

मुकुलिका आर: 1897 के महामारी रोग अधिनियम ने प्लेग पासपोर्ट, छूट प्रमाणपत्र और यहां तक कि नज़रबंद जैसे कई चिकित्सा निगरानी उपायों को लागू किया था। पिछले महीने उसी औपनिवेशिक अधिनियम को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू किया गया, जो मौजूदा महामारी से निपटने के लिए उसी तरह के निरीक्षण और अलगाव की मंज़ूरी देता है। असल में आईटी विशेषज्ञों ने कथित गोपनीयता / डेटा उल्लंघन के लिए केंद्र सरकार के मोबाइल एप्लिकेशन,”आरोग्य सेतु” को लेकर चिंता जतायी है। क्या महामारियां सुपर निगरानी करने वाले राष्ट्रों या “कोरोनोप्टीकॉन” राष्ट्र के निर्माण के फलने-फूलने में अपनी भूमिका निभाती हैं और अगर ऐसा है,तो वह किस तरह होता है?
रोमिला थापर: मैं 1897 के महामारी रोग अधिनियम और उसके बाद के प्रभावों के बारे में बहुत कम जानती हूं। मेरा जो अध्ययन क्षेत्र है, वह है सुदूर अतीत का इतिहास, और बेशक उस इतिहास में ऐसा कोई क़ानून नहीं था। लेकिन, 123 साल पहले पारित किये गये एक अधिनियम को लागू करना ऐतिहासिक समझ की कमी की ओर इशारा तो करता ही है, इससे मेरा मतलब यह है कि समाज और प्रौद्योगिकियां बदलते रहते हैं और ऐसे में उन्हें स्थिर मानकर बहुत पहले के उस क़ानून को भला कैसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, इन दिनों सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों की सोच बहुत हद तक औपनिवेशिक मान्यताओं में निहित है, ऐसे में हैरानी की बात नहीं है कि उसी तरफ़ कुछ-कुछ मुड़ता हुआ सा दिख रहा है। किसी इतिहासकार को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि 123 वर्षों में न सिर्फ़ सरकार की प्रणाली बदल गयी है, बल्कि तकनीक और जिस तरह से उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, वह भी बदल गया है। अब हमारी सरकार सत्तावादी औपनिवेशिक सरकार नहीं है और हम इस बात को कहते रहते हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं।
आमतौर पर लोकतंत्र सामान्य निगरानी से परे किसी भी चीज़ पर अपने कार्यप्रणाली को आधारित नहीं करता है, इसके लिए उसे उन्नत तकनीक की ज़रूरत नहीं होती है। निगरानी उपाय या उस मामले को लेकर किसी अन्य तरह की व्यवस्था को सबसे अच्छे तरीक़े से नहीं थोपा जा सकता है, जैसा कि 1897 में थोपा गया था। जब तक कि नतीजे कुछ विस्तार के साथ सामने नहीं आ जाते, तबतक व्यवस्थायें नहीं पलटी जा सकती हैं। शुरुआती लॉकडाउन को लेकर जो व्यवस्था बनायी गयी थी, उसमें ऐसा पर्याप्त रूप से नज़र आया था, और ऐसा इसलिए हुआ था,क्योंकि जो व्यवस्था बनायी गयी थी, उसे बनाने पर न तो पर्याप्त समय दिया गया था और न ही उस पर पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श किया गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के लिए भारी समस्यायें पैदा हो गयी हैं। ये वही समस्यायें हैं, जिनका सामना हमें इस समय सबसे पहले करना पड़ रहा है।
1897 में निगरानी को लेकर व्यक्तिगत पूछताछ के आधार पर कुछ क़ाग़ज़ी कार्रवाई होती थी और यह कार्रवाई सभी को लेकर होती थी। आज की ‘आरोग्य सेतु’ ऐप मौजूदा तकनीक पर आधारित है, जो किसी व्यक्ति के जीवन और गतिविधियों पर गहनता से जांच-पड़ताल कर सकती है, जो 1897 के अधिनियम में संभव नहीं था। और निश्चित रूप से कोविड-19 रोगी या संभावित रोगी की जांच में जो कुछ ज़रूरी है, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या हम उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, जो इस समय जांच-पड़ताल कर रहे हैं, इस तरह की जांच-पड़ताल क्या आगे नहीं होगी ?
लॉकडाउन की प्रतिक्रिया अपने दूर-दराज़ के गांवों में वापसी के लिए सड़कों पर चल रहे लाखों लोगों की सबसे ख़राब हालात में साफ़-साफ़ दिख रही है। कोई भी संवेदनशील मानवीय व्यवस्था घर जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए परिवहन, भोजन और आश्रय का इंतज़ाम तो की ही होती। लेकिन, ऐसा करने के लिए उसे संख्याओं या सामूहिक मज़दूर के तौर पर नहीं, बल्कि हम सभी की तरह उन्हें भी पुरुषों और महिलाओं के रूप में देखना होगा। बुनियादी ज़रूरतों और आजीविका के नियमित साधनों के बिना लोग अब अलग-अलग तरीक़ों से अपने जीवन में भारी संकट का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपने घर जाने जैसी मामूली इच्छा पर न तो किसी हुक़्म से दबाव बनाया जा सकता है और न ही उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है। उन्हें ज़बर्दस्ती रोके जाने का प्रयास किया जा रहा था और ऐसा इसलिए, क्योंकि उनके जाने से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। क्या भारतीय नागरिक इतना भी स्वतंत्र नहीं हैं कि वे ख़ुद इस बात का चुनाव कर सकें कि वे कहां और कैसे रहना चाहते हैं ?
इस बात को जानते हुए कि वे कई दिनों से सड़कों पर थे और उनके पास पैसे तक नहीं थे, इसके बावजूद उन्हें ट्रेन पर चढ़ने के लिए ट्रेन का किराया देने को कहा गया। अनाज, जो अनाज के गोदामों में भरा पड़ा है, क्या उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा सकता था। ये हालात क्यों हैं, इस पर बहुत कम बातें हुई हैं। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाय कि इंसान होना और समाज में रहना ही सुशासन के तहत होना माना जाना चाहिए। कोई भी इस बात का आसानी से अनुमान लगा सकता था कि लॉकडाउन में बिना खाने-पीने और बिना मज़दूरी वाले लोग ही उन लोगों में से पहले होंगे, जो वहां जाना चाहेंगें, जहां उन्हें लगा होगा कि भोजन और आश्रय मिलेगा और कोई शक नहीं कि ऐसी जगह उनके गांवों में उनके अपने घर हैं।
मुकुलिका : इतिहासकार बताते हैं कि औपनिवेशिक बॉम्बे में प्लेग विरोधी उपाय हर तरह के दमन (ग़रीबों को तंग करने) और सामाजिक-राजनीतिक आधिपत्य (पश्चिमी चिकित्सा आदि) को स्थापित किये जाने के हथियार बन गये थे। ठीक इसी तरह, यह भी तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रवादी बहस के हिस्से के रूप में ऐसे शहरों में महामारी को रोकने के लिए चिकित्सा सहित उन औपनिवेशिक उपायों के प्रतिरोध के ज़रिये नवजात हिंदू चेतना की नींव भी रखी गयी थी। क्या आप मौजूदा महामारी के सिलसिले में उसी तरह की आधिपत्य वाली बहस में हो रही बढ़ोत्तरी को नहीं देख पा रही हैं?
रोमिला थापर: जहां तक आधिपत्य वाली बहस का सवाल है, तो इसका स्वाद तो हम पहले ही चख ही चुके हैं, जिसका असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसे अलग-अलग मौक़ों पर किस तरह ज़ाहिर किया गया है, इसे समझकर एक बड़ी समझ को विकसित किया जा सकता है, ये मौक़े थे- तबलीग़ी जमात के आयोजन के बाद; उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आयोजित दंगों के दौरान और उसके बाद; राजनेताओं के भाषणों में गोली मारने का आह्वान। महामारी के आने के साथ ही जिस तरह की बहस शुरू हो गयी थी, वह यह एक ऐसी बहस है,जो जल्दी फ़ीकी नहीं पड़ेगी। एक दूसरी तरह की बहस से उत्तर-पूर्व के उन लोगों को लेकर चिंता पैदा होती है, जिनके ख़िलाफ़ शत्रुता का भाव भी है। क्या ऐसा सिर्फ़ इसलिए है,क्योंकि जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि वे अलग दिखते हैं, या फिर इसलिए भी है कि उनमें से बहुत सारे लोग ईसाई हैं?
मुकुलिका : एक तरफ़ हमने देखा है कि इस तरह के संकटों के समय किस तरह लोग बलि का बकरा बना दिये जाते हैं और कुछ पूर्वाग्रहों के शिकार हो जाते हैं (यूरोप में प्लेग के दौरान यहूदी; भारत में मुसलमान और अमेरिका में अश्वेत; हैजे के प्रकोप के दौरान भारत के ख़िलाफ़ नस्लवाद, और इस समय चीन के ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है) और दूसरी तरफ़ शक्ति समीकरण (वर्ग, लिंग आदि) किस तरह मज़बूत हो जाते हैं। क्या आप इस हालात की व्याख्या कर सकती हैं?
रोमिला थापर: सत्तावादी व्यवस्था के लिए बलि के बकरे का होना ज़रूरी होता है। किसी ऐसे समुदाय को चुन लिया जाता है, जिसे ऐतिहासिक समय से ही दुश्मन क़रार दिया जाता है, और इसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती है। उस समुदाय का विरोध व्यवस्था को दूसरों को भी ऐसा ही करने का अवसर देती है, ख़ासकर उन लोगों को,जो बलि का बकरा होने पर आपत्ति जताते हैं। जर्मनी में नाज़ी शासन के तहत यहूदियों के उत्पीड़न में यह साफ़ तौर पर नज़र आया था, क्योंकि वास्तव में ऐसा हर कहीं होता रहा है। अब तो यह एक जाना-पहचाना पैटर्न है।
मुकुलिका: कई लोगों का मानना है कि महामारियां जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को प्रेरित करते हुए इतिहास के सिलसिले को बदलने और नयी दुनिया को खोलने में सक्षम होती हैं,अक्सर कहा जाता है कि यूरोपीय पुनर्जागरण प्लेग के चलते हुई तबाही के कारण हुआ था। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि महामारी एक ज़रिया है ?
रोमिला थापर: सच्चाई तो यही है कि समाज के रूप में हम अब भी अपने विभिन्न ऐतिहासिक सफ़र में हैं, और इस सफ़र के रास्ते और उन रास्तों में जो कुछ बदलाव हुए हैं, उनकी व्याख्या इतिहासकारों द्वारा महामारी को ज़्यादा अहमियत दिये बिना ही की गयी है, इससे तो यही पता चलता है कि कोई महामारी इतिहास को इतना ज़बर्दस्त रूप से भी नहीं बदल सकती है। लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों को छोड़कर ज़्यादातर इतिहासकारों ने अब तक महामारी के बाद के प्रभावों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ़्लू जैसी ज़्यादातर पिछली महामारियां भौगोलिक रूप से एक या दो महाद्वीपों तक ही सीमित रही हैं। कोविड-19 का फैलाव ज़्यादा व्यापक है। और इस महामारी से आगे चलकर इसकी चपेट में वैश्विक अर्थव्यवस्था भी आ गयी है।
तीन ऐसे क्षेत्र हैं,जिनमें इस महामारी से बदलाव आने की संभावना है:
1. वैश्वीकरण और नवउदारवाद की आलोचना ख़ूब हुई है और उम्मीद की जा सकती है कि इसे छोड़ दिया जाये ताकि हूक़ूमत वह कर सके, जो उसे करना चाहिए था, यानी हर समय सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। जो भी सरकार सत्ता में है, उसे सभी के लिए भोजन, पानी, नौकरी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक न्याय की गारंटी और उन्हें बनाये रखना होगा। इसके लिए सभी सरकारों और उनके कामकाज की व्यापक निगरानी की ज़रूरत हो सकती है। असल में समस्या ऐसे लोगों के नहीं होने की है, जो इस तरह की निगरानी कर सके। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास शक्ति का अभाव है। आख़िरकार शक्ति तो उन्हीं लोगों से मिलती है, जिन पर शासन किया जा रहा होता है, और नागिरकों के तौर पर जिनके पास राज्य के कामकाज पर सवाल उठाने का अधिकार होता है। सवाल है कि क्या उन्हें असरदार तरीक़े से ऐसा करने दिया जायेगा?
2. ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को तुरंत लागू किया जाना चाहिए,जिसके भीतर सभी नागरिकों आते हों। इसके बिना यह महामारी स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की मौजूदा कमी के चलते कुछ वर्षों तक हमारे आस-पास बनी रहेगी। यह बात न सिर्फ़ इस महामारी से सुरक्षित रख-रखाव पर लागू होती है, बल्कि उस बुनियादी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराये जाने पर भी लागू होती है, जो महामारी के प्रसार को रोकती है।
3. पर्यावरण की सुरक्षा अहम है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को सरकारी एजेंसियों और निजी उद्यमों के अतिक्रमण से संरक्षित और सुरक्षित किया जाना ज़रूरी है। यह वायरस प्राकृतिक जीवन और पशु जीवन के दुरुपयोग से पैदा हुआ है और इस दुरुपयोग को रोकना होगा, अन्यथा हम किसी दूसरे वायरस का भी शिकार हो सकते हैं।अगर हम अपने संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करें, तो ये सारे उपाय किये जा सकते हैं। जैसा कि हम प्रवासियों के मामले को ले सकते हैं, बिना दस्तावेज़ वाले लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर के निर्माण के बजाय हमें अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करना चाहिए। बिना किसी तुक के दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा पर नये गगनचुंबी इमारत के निर्माण के बजाय, उन्हीं पैसों से घर बनाकर और पानी की आपूर्ति करके उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान दिया जा सकता है, जो ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। सरकारों को इस बात की याद दिलाते रहना होगा कि उनका मूल्यांकन उन लोगों के लिए किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों से होगा, जिन पर वे शासन करते हैं। एक खाता-पीता पर्यटक ही किसी स्मारक से प्रभावित हो पायेगा, एक भूखा दिहाड़ी मज़दूर, जिसे उसकी मज़दूरी भी नहीं मिली हो, वह किसी स्मारक की परवाह भला क्यों करेगा।