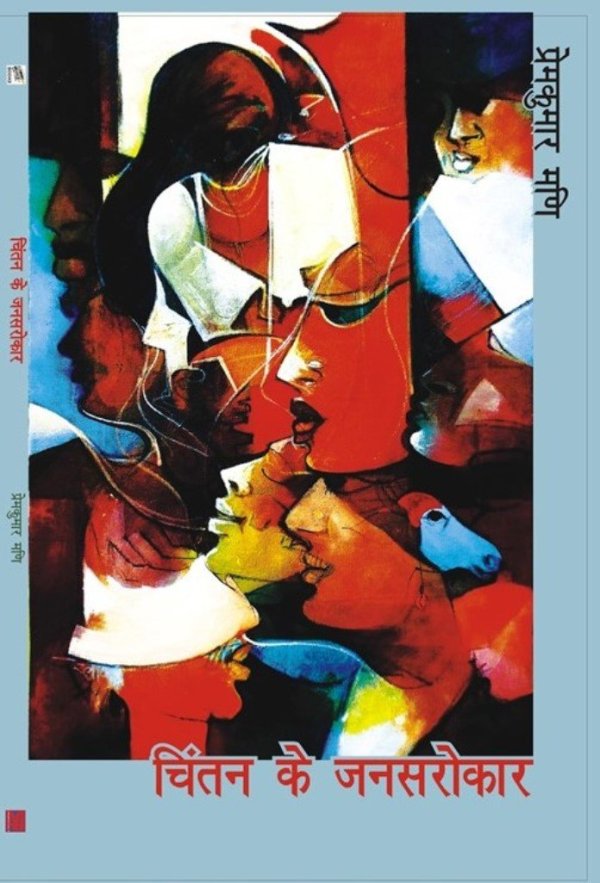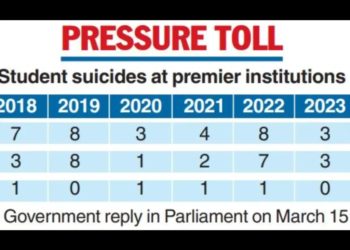किसी किताब की यह सफलता होती है कि वह अपने पाठक को इतना उद्वेलित कर दे कि वह अपने परिवेश और जीवन के हर पहलू पर फिर से विचार करने को विवश हो जाय। ऐसे ही लेखों का संकलन है ‘चिंतन के जनसरोकार’। हिन्दी के महत्वपूर्ण लेखक प्रेमकुमार मणि के प्रमुख लेखों का यह एक संकलन है।
भारतीय हिन्दू समाज में चिंतन की जो धारा है अमूमन हमारा विचार भी उसी धारा की दिशा में प्रवाहित होता रहता है। जाति के जिस पायदान पर कोई खड़ा है उसी से उसकी जीवन धुरी चलती रहती है। वो कितनी सारी बातों को सहज मान कर जीवन जीता जाता है। उसकी चिंतन प्रक्रिया भी निर्बाध रूप में चलती जाती है। यह प्रकिया तभी रूप बदलती है जब यथार्थ का कोई इतर रूप व्यक्ति के सामने टकराये। दुर्भाग्यवश ज्यादातर मामले में यह एक्सीडेंटल ही होती है।
खैर यह जरूरी हो जाता है कि वह ठहर कर अपने चिंतन के तरीके और सरोकारों पर सोचे। उसके सरोकार क्या हैं, वह खुद नहीं बता सकता। उसने अब तक जिन चीजों का अभ्यास किया है, जिसको उसने बिना प्रश्नवाचक लगाये मान लिया है उसको फिर से सवालों के घेरे में खड़ा करना तक इस प्रक्रिया में शामिल है।
इसी किताब से हमें समझ आता है कि हमारी परम्परा में चिंतन की दो धारा हमेशा से मौजूद रही है। लेकिन अंधेंरे की धूल भरी आंधी ने उसको ढ़क दिया। दूसरी धारा कमजोर हो गयी। उसको समझना ही कमजोरी की निशानी बना दी गई। चिंतन की दो धाराएं थीं- “एक है ब्राह्मण परम्परा दूसरी है श्रमण की परम्परा। हमारे शब्दकोष बताते हैं कि श्रमण का अर्थ है-परिश्रमी, मेहनती व संन्यासी और ब्राह्मण का अर्थ है चैतन्य। जन्मना जायते शूद्र संस्कारै द्विज उच्चते यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार किसी को द्विज बनाता है। द्विज के शीर्ष पर ब्राह्मण हैं- पूर्णचैतन्य ”। अब किसी को पूर्ण चैतन्य अवस्था में पहुंचने के लिए विशिष्ट भौतिक परिस्थितयों की आवश्यकता होती है। इस भौतिक परिस्थिति की पहली अनिवार्यता है कि व्यक्ति श्रम से कटा हो। वह शारारिक श्रम से बहुत दूर हो। इसलिए हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शारारिक श्रम को बेहद हिकारत से देखा जाता है। जो जितना कम परिश्रम करता है वो उतने ऊंचे पायदान पर उपस्थित है। आज श्रमण की परम्परा बहुत ही कमजोर है या कहें कि उसकी परम्परा को आत्मसात करके उसको साहस के साथ स्वीकार करके विकसित करने का जिम्मा चिंतको ने छोड़ दिया है। बल्कि चिंतन का अर्थ ही बाह्मण परम्परा को विकसित करना हो गया और संस्कार का अर्थ तो केवल जनेऊ संस्कार बन चुका है।
यह लेख एक नजरिया देता है अपने मिथकों या सामयिक मुद्दों को समझने के लिए। चाहे बात समुद्र मंथन के दौरान देवताओं का असुरों को चालाकी से नाग वासुकी का मुख पकड़ाया जाना हो या मंथन के बाद एक स्त्री (भोग्या के रूप में) का इस्तेमाल करके अमृत का चालाकी से बंटवाना हो। यह सब एक सत्य का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं जिस पर शोर मचाकर चुप कराने से कुछ हासिल नहीं होगा। कथा के भी कई पक्ष होते हैं कथा के भीतर एक अन्तरकथा होती है उसका स्वर कोई भी अपने सरोकारों के माध्यम से ही पकड़ सकता है।
प्रेमकुमार मणि ने अलग-अलग आलेख लिखे हैं। गांधी से ज्यादा आंबेडकर का भारत या उदार भारत में दलित या आरक्षण का सवाल हो, वह अपने सभी आलेखों में बहस से ज्यादा उक्त विषयों में नजरिये के सवाल पर प्रश्न खड़ा करते हैं। अपने एक लेख में वह आंबेडकर के कार्टून वाले विवाद पर बेहद स्पष्ट नजरिया प्रकट करते हैं “..मैं नहीं समझता कि कार्टून में बाबा साहेब के लिए अपमान की कोई बात है। अपमान की बात है, कार्टून को विमर्श से बाहर कर देना। (जिसकी घोषणा हो चुकी है) कुछ लोग फुले, आंबेडकर, पेरियार जैसे लोगों को इतिहास और विमर्श का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते। हमें यह समझना चाहिए कि कला, विज्ञान और साहित्य जैसे विषयों मे आपका शत्रु वह नहीं होता, जो आपको आलोचना के लिए चुनता है, बल्कि शत्रु वह होता है, जो आप पर चुप लगा जाता है”। उनके सारे लेख ब्राह्मणवादी चिंतन प्रक्रिया पर प्रहार करते हैं
यह जरूर है कि जहां वो पब्लिक सेक्टर की खराब हालत की बात करते हैं वहां उनकी सीमाएं भी दिखती है। वो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की नियुक्तियां हुई और चूंकि वो अकुशल श्रमिक थे इसलिए उसकी बदहाली हुई। जहां तक उदारीकरण या निजीकरण का प्रश्न है उसके कारण अलग हैं। लेकिन हां श्रम की संस्कृति का अभाव होने के चलते विभिन्न विभागों में साहबी ठाठ जरूर रहा और परिणामस्वरूप जनता इस प्रक्रिया से बहुत उद्देलित भी नहीं हुई।
अपने विभिन्न लेखों में प्रेमकुमार मणि जी साहित्य राजनीति की उन तमाम गुत्थियों की तरफ इशारा करते हैं जिनका खुलना आवश्यक है। वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपंन्यास गोरा के नायक के उस अंतिम दृश्य से गांधी के जीवन के अंतिम पड़ाव की तुलना करते हैं जहां गोरा के सामने जीवन का राज खुल चुका है वो जान चुका है कि पवित्रों की इस दुनिया में वह स्वयं अपवित्र है। वह आत्मबोध से तत्वबोध की यात्रा करता है। वह स्वंय को उस स्थान पर पाता है जहां वह बहुजन के साथ एका बनाये या फिर कुंठा के दलदल में तिरोहित हो जाय। प्रेम शंकर कहते हैं कि “गोरा का संघर्ष गांधी का संघर्ष है। गोरा के रूप में हम एक भारत व्याकुल हिंदू गांधी को ही पाते है। गांधी को भी यह तत्वबोध अपने जीवन के आखिरी काल में हुआ था और यही कारण था कि वह एक रूढ़ हिंदू की गोलियों के शिकार हुए”।
इसी पुस्तक में रवींद्र स्मरण में वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1920 में अपना उपन्यास घरे-बाइरे लिखा और उसमें गांधी के असहयोग आंदोलन पर व्यंगात्मक तीर चलाए, तब भी गांधीवादियों की ओर से आपत्तियां दर्ज की गई थीं। लेकिन रवींद्रनाथ ने अपने व्यक्त विचारों के लिए खेद प्रकट नहीं किया। आज कहा जा सकता है कि रवींद्र ने उस आंदोलन को ज्यादा सही ढ़ंग से समझा था।
इस पूरी किताब में चाहे कई महत्वपूर्ण लोगों को याद किया गया है। किन्तु व्यक्तियों के प्रति कहीं से भी बैरभाव या दुराग्रह नहीं झलकता। बल्कि उन व्यक्तियों की वैचारिकी और उसकी सीमाओं को बखूबी रेखांकित किया गया है। चाहे वो बाल ठाकरे की बात कर रहे हों या लालू यादव की। इसी क्रम में, श्रीलाल शुक्ल भीड़ के लेखक नहीं थे शीर्षक लेख में वे कहते हैं कि – “राग दरबारी को हिंदी साहित्य के चार महत्वपूर्ण उपन्यासों में माना जाता है। इसके साथ प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी और रेणू का मैला आंचल है। वो कहते हैं कि अगर मैला आंचल, गोदान और रागदरबारी को एक साथ रखें तब एशियाई समाज की वे आर्थिक सामाजिक स्थितियां हमारे सामने साकार होने लगती हैं जिसे गुन्नर मिर्डल ने अपने एशियन ड्रामा में बतलाना चाहा है। कार्ल मार्क्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय ग्रामों को काव्यात्मक ग्रामीण बस्तियां कहा था। एक लंबी व्याख्या के साथ इसे पूरब की निरंकुशता (ओरियंटल डिस्पाटिज्म) का आधार भी कहा था। मैं कह सकता हूं कि हिंदी के ये तीनों उपन्यास चुपचाप मार्क्स के निष्कर्षों के समर्थन में खड़े दिखते हैं। गोदान का होरी, मैला आंचल का बावनदास और रागदरबारी का लंगड़ एक ही बात बतलाते दिखते हैं। इनकी समन्वित चेतना देखने में चाहे जितनी निर्गुण प्रतीत होती हों, अपने समय की मुख्य राजनीतिक चेतना गांधीवाद से विद्रोह करती दिखती है। गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी और जिसे साकार करने में गांधीवादियों ने खुद को ‘समर्पित’ कर दिया, वह नतीजे के तौर पर एक महापाखंड के रूप में अवतरित हुआ, जिसकी शिनाख्त मैला आंचल और रागदरबारी बखूबी करते हैं। बावनदासकी की भारतमाता जार-जार रो रही हैं और लंगड़ अपने जनतंत्र से अपनी तरह लड़ रहा है”।
यह बहुत ही अटपटी स्थिति है कि लेखक के विचार बिना जाने उसे हाशिये पर ठेल दिया जाय। बीते दिनों प्रेमकुमार जी के लेख ‘किसकी पूजा कर रहें हैं बहुजन’ पर बहुत विवाद हुआ। ज्यादातर लोगों ने वह लेख पढ़ा नहीं होगा लेकिन पूर्वाग्रह के चलते उसपर कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं किया। दरअसल यह लेख भी चिंतन की क्षीण हो चुकी धारा यानि श्रमण की ताकत से पैदा हुआ है। कथा हो या मिथक, न्यायोचित प्रश्न खड़े होना लाजिमी है। उनका यह लेख शक्तिपूजा की शुरूआत आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के अंतर और उसके सामंजस्य से पैदा हुए मिथकों पर राय प्रकट करता है। यह कहीं से भी स्त्री-विरोधी नहीं है।
प्रेमकुमार मणि (1953) हिंदी के प्रतिनिधि कथाकार व चिंतक हैं। उनके चार कथा संकलन अंधेरे में अकेले (1990) घास के गहने (1993) आदि हैं उनका उपन्यास ढलान (2000) प्रकाशित हुआ है। कथा लेखन के लिए वे श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। उनकी पहचान एक समाज-राजनीतिकर्मी के रूप में भी है।
First published in Forward Press